(जॉक लकान के मनोविश्लेषण के सिद्धांतों पर केंद्रित एक विमर्श की प्रस्तावना)
—अरुण माहेश्वरी
जाक लकान
(13 अप्रैल 1901 — 9 सितंबर 1981)
(7)
मनुष्य का सामान्य स्वातंत्र्य बोध और लकान
असामान्य, मनोरोगी कहलाने वाले मनुष्य के सच को जानने के लिये कि हमारे सामान्य की संरचना क्या है, यह एक जरूरी सवाल है और इसके साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि असामान्य कैसे उस संरचना की ही अपनी कमियों के साथ जुड़ा हुआ है । इसे समझने के लिये लकान के मनोविश्लेषण के सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं । यह समझ मनुष्य के व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों की ऐसी कुंजी है जिस पर अधिकार करके उसे उसकी समग्र प्राणीसत्ता पर आरोपित बाह्य बाधाओं से अधिक से अधिक मुक्त किया जा सकता है । इसीलिये यह हमारे पतंजलि के योग दर्शन की तरह ‘योगश्चितवृत्ति निरोध’, अर्थात् चित्त की वृत्तियों का निरोध, अर्थात् महज एक चिकित्साशास्त्र नहीं है । यह वह है जिसे हमारे अभिनवगुप्त भैरव भाव की साधना बताते हैं — जिसके अंत में आदमी में लालसाओं का कोई अंत नहीं होता लेकिन 'अन्य' किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती । आवरणरहित शुद्धप्रकाशमय । ‘तस्य स्वामी संसारवृत्तिविघटनमहाभीमः ।’ (वह संसारवृत्ति के विघटन में महाबलशाली स्वामी ) आदमी के परम स्वातंत्र्य की प्राप्ति का परम भाव, अन्य की उपस्थिति के दबाव से इंकार का भाव । मार्क्स का सर्वहारा जो कोई एक ठोस वर्ग नहीं, जैसा कि आम तौर पर कम्युनिस्टों के बीच मजदूर वर्ग को मान लिया जाता है, बल्कि मनुष्य की परम मुक्ति का एक भाव है, वह भाव जो समूचे समाज की मुक्ति की प्रक्रिया का वाहक होता है । मजदूर वर्ग को सर्वहारा का पर्याय मान लेने से समाजवादी आंदोलन में जितने विचारधारात्मक विभ्रम पैदा हुए हैं, उनका कोई अंत नहीं है । (देखें, अरुण माहेश्वरी, समाजवाद की समस्याएं, ‘हम भी इक अपनी हवा बांधते हैं : प्रसंग ‘वर्गीय राजनीति’)
आज की बौद्धिक दुनिया में जाक लकॉन के अनुयायियों की एक पूरी सेना बन चुकी है । अभी के विचारधारात्मक, दार्शनिक और साहित्य संबंधी नये सिद्धांतों की चर्चा करने वाले तमाम लोग इस फ्रांसीसी मनोचिकित्सक पर सिर्फ किसी मनोविश्लेषक के रूप में नहीं, बल्कि एक श्रेष्ठ दार्शनिक के रूप में, एक भाषाशास्त्री के रूप में, यथार्थ के भ्रमों को अपसारित करके विषय के तल तक जाकर उसे उलट देने के क्रांतिकारी तत्वमीमांसक, विचारक के रूप में भी चर्चा करते हैं । जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, आज के वक्त के सबसे प्रमुख कम्युनिस्ट दार्शनिक एलेन बाद्यू बड़े सम्मान के साथ लकान का नाम लेते हैं तो लोकप्रिय मार्क्सवादी दार्शनिक स्लावोय जिजेक बात-बात पर लकान के मनोविश्लेषण के निष्कर्षों का उल्लेख करने से नहीं चूकते । जिजेक अपने को घोषित रूप से लकान के अनुयायियों की कतार में भी शामिल करते हैं ।
पूरे पश्चिमी जगत में लकान की यह प्रतिष्ठा उनके जीवित काल में ही न सिर्फ मनोविश्लेषण के जगत में, बल्कि दर्शनशास्त्र और आदमी के चित्त के जगत पर चर्चा के तमाम संदर्भों में हो गई थी । उन्होंने अपने जीवन के लगभग साठ से भी ज्यादा वर्ष फ्रायड की तरह ही बाकायदा एक मनोचिकित्सक के रूप में बिताये और उसी क्रम में मनुष्यों के चित्त जगत के विचित्र-विचित्र रूपों के पर्यवेक्षण से आदमी के चित्त की गति-प्रकृति के बारे में जो निष्कर्ष निकाले । इन्हीं कारणों से वे चरक संहिता की भारतीय कहावत 'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' को चरितार्थ करते हुए मानव मन और समाज की गति-प्रकृति पर चर्चा के लिये सर्वकालिक महत्व के माने जाते हैं । पश्चिम में क्रमशः उनकी चर्चा हेगेल, किर्केगार्द, मार्क्स, हाइडेगर की श्रेणी के दार्शनिकों और सार्त्र, दरीदा आदि के स्तर के बुद्धिजीवियों, विचारकों और शिक्षकों की श्रेणी में भारी आदर के साथ की जाती है ।
लकान के जीवित काल में बहुत से लोग अपने को लकानपंथी अर्थात लकान के अनुयायी कहने लगे थे, लेकिन खुद लकान अपने बारे में कहते थे कि कोई भी अपने को मेरा शिष्य कहने के लिये स्वतंत्र है, लेकिन मैं खुद फ्रायड का चेला हूं । यद्यपि यह भी सच है कि अपने जीवन के अंतिम सेमिनारों में वे मार्क्स की सबसे ज्यादा चर्चा करते थे । मार्क्स को लक्षणों का आविष्कारक कह के उन्होंने एक प्रकार से एंगेल्स की उस बात पर ही मोहर लगाई थी कि मार्क्स ने किसी वैज्ञानिक की तरह सामाजिक परिवर्तन के नियमों की खोज की थी । (देखें - SAMO TOMŠIČ, THE CAPITALIST UNCONSCIOUS : MARX AND LACAN , VERSO, New York)
गौर करने लायक है सैमो तौजिक का यह कथन जिसमें वे कहते हैं — “मार्क्स लक्षणों के पहले सिद्धांतकार थे, ऐसा कहने का अर्थ है कि सर्वहारा अचेतन का विषय है । अर्थात् सर्वहारा का मतलब एक ठोस सामाजिक वर्ग से कहीं ज्यादा है । यह पूंजीवाद में एक सर्वकालिक आत्म स्थिति को दर्शाता है । लेकिन एक लक्षण की तरह ही, अर्थात ऐसे विन्यास की तरह जिससे वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का दमित सत्य राजनीति के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ता है, सर्वहारा पूंजीवाद के द्वारा लाद दी जा रही झूठी और अमूर्त सार्विकता को ठुकराता है, जिसे माल के रूप की सार्विकता कह सकते हैं । (इसे ही हमने तंत्र की भाषा में भैरव भाव कहा है — अ.मा.) सर्वहारा को एक ठोस रूप के बजाय अचेतन के विषय के रूप में देखने से वर्ग संघर्ष की धारणा और सच्चाई भी एक भिन्न रूप में सामने आते हैं । वह अब महज वर्तमान के वास्तविक सामाजिक वर्गों के बीच संघर्ष को व्यक्त नहीं करता है बल्कि सामाजिक और आत्मिक जगत में ढांचागत अन्तर्विरोधों को व्यक्त करता है, और इस प्रकार अचेतन की तरह का ही ज्ञानमीमांसक-राजनीतिक रूप ले लेता है । न वर्ग संघर्ष और न अचेतन ही कोई इतिहासव्यापी अभेद सत्य है — इनकी पूरी ‘संगति’ इनके प्रत्यक्ष रूपों के विरूपीकरण में निहित होती है, जो विरूपीकरण किसी भी व्यवस्था के पुनर्उत्पादन में देखने को मिलता है ।
“मार्क्स और लकान नकारात्मकता और सकारात्मकता के बीच, मृत और जीवित श्रम के बीच, अमूर्त ढांचे और ठोस अनुभव के बीच, विन्यास और उत्पत्ति के बीच किसी साधारण विरोध को अस्वीकारते हैं ।
(That Marx was the first theoretician of the symptom implies that the proletariat is the subject of the unconscious. This means that the proletariat designates more than an empirical social class. It expresses the universal subjective position in capitalism. But as a symptom, that is, as a formation through which the repressed truth of the existing social order is reinscribed in the political space, the proletariat entails a rejection of the false and abstract universalism imposed by capitalism, namely the universalism of commodity form. With the shift from the proletarian seen simply as an empirical subject to the subject of the unconscious, the notion and the reality of class struggle also appears in a different light. It no longer signifies merely a conflict of actually existing social classes but the manifestation of structural contradictions in social and subjective reality, thereby assuming the same epistemological-political status as the unconscious. Neither class struggle nor the unconscious stands for some invariable transhistorical essences – their entire ‘consistency’ lies in the distortion of appearances that accompany the reproduction of the given order.
Marx and Lacan reject the simple opposition between negativity and positivity, dead and living labour, abstract structure and concrete experience, structure and genesis. )
दरअसल, नियम ही तो लक्षणों के रूप में क्रियाशील होते हैं और खास परिस्थितियों में ठोस यथार्थ का स्वरूप लेते हैं । इस खास परिस्थिति के लिये ही लकान का शब्द था — Topology (स्थानिकता) । हर लक्षण के ठोस रूप में प्रकट होने की अपनी स्थानिकता होती है । मार्क्स ने जब पूंजी में पण्य के दो रूपों, उसके ठोस वस्तु रूप और मूल्य रूप की बात कही थी, तब वे उसके स्वरूप की लाक्षणिकताओं को ही व्यक्त कर रहे थे और उनका साफ कहना था पण्य के मूल्य का निर्धारण “व्यवहारिक उद्देश्य के लिये इस्तेमाल की जाने वाली एक काम चलाऊ तरकीब” होती है, अर्थात् इसका कोई ठोस आधार नहीं होता, लेकिन यह सत्य होता है । अर्थनीति का ताना-बाना उसी अगोचर परातत्व के यथार्थ से बुना जाता है । पूंजीवादी अचेतन से पूंजी का सच व्यक्त होता है ।
बहरहाल, फ्रायड के बारे में लकान का पहला वाक्य था — “उन्होंने एक विज्ञान की स्थापना की थी ।” मनोविज्ञान जो मनुष्य की वासनाओँ की जानकारी तक सीमित था, उसे उसके अपने लक्ष्य की सापेक्षता में रखना ही तो उसे विज्ञान बना देता है । लकान के शब्दों में, “अन्य किसी क्रांति की तरह ही फ्रायडीय क्रांति भी अपने संदर्भ से अपना अर्थ ग्रहण करती है, उस समय के मनोविज्ञान में जो प्रचलित था, उसके संदर्भ से ।” (Jacques Lacan, Ecrits, The first complete edition in English; W. W. Norton & Company, Page – 59) यह वैसा ही है जैसा मार्क्स के बारे में एंगेल्स ने कहा था कि वे “मानव इतिहास के विकास के नियम का पता लगाने वाले वैज्ञानिक थे”।
मार्क्सवादी चिंतक लुईस आल्थुसर का एक लेख है — Freud and Lacan । इसमें वे फ्रायड और विज्ञान के प्रसंग को बड़े दिलचस्प अंदाज में उठाते हैं । वे लिखते हैं कि पश्चिमी तर्कशास्त्र के इतिहास में आदमी की हर जरूरत, उसकी दूरदृष्टि, उसकी सजगता और सचेतनता को वंशपरंपरा से जोड़ा जाता है । (जैसे भारत के शैव दर्शन में क्रम सिद्धांत है — अ.मा.) इस प्रकार का जन्मजात कारण यहां एक सांस्थानिक रूप ले चुका है । जब भी कोई नया विज्ञान पैदा होता है, उसका वंशानुगत क्षेत्र शुरू में हमेशा अचरज, खुशी और फिर उसके उपनयन तक के लिये आकुल रहता है । लंबे काल तक प्रत्येक शिशु को, वह बिल्कुल नादान होने पर भी, उसके बाप का बेटा कहा जाता है । पर जब वही शिशु प्रतिभाशाली, तीक्ष्ण बुद्धि वाला नौजवान बन जाता है, उसका पिता ही उससे लड़ने के लिये घर के दरवाजे पर खड़ा तैयार मिलता है, बस बेटे के प्रति मां की भावना का लिहाज करके थोड़ा काबू में रह जाता है । हमारे इस भीड़ भरे जगत में जन्म पाने के लिये जगह होती है, बच्चे के बारे में भविष्यवाणी के लिये जगह होती है, लेकिन उसके भविष्य के लिये !”
आल्थुसर इस विस्मयपूर्ण सवाल के साथ कहते हैं कि “मेरी जानकारी में 19वीं सदी में सिर्फ दो या तीन ऐसी संतानें पैदा हुई है जिनकी पैदाईश की कोई उम्मीद नहीं की गई थी । मार्क्स, नित्शे और फ्रायड । ये प्राकृतिक संतानें इसलिये क्योंकि प्रकृति किसी परंपरा की, सिद्धांतों, नैतिकता और सदाचारों की गुलाम नहीं हुआ करती है ; प्रकृति का अर्थ है अस्वीकृत नियम — जैसे अविवाहित मां, अर्थात् कानूनी पिता की अनुपस्थिति । पश्चिमी विवेक पितृ-विहीन बच्चों से भारी कीमत अदा करवाता है । मार्क्स, नित्शे और फ्रायड को जिन्दा रहने के लिये बिल्कुल अमानवीय कीमत अदा करनी पड़ी थी — वहिष्कार, निंदा, अपमान, गरीबी, भूख और मृत्यु अथवा विक्षिप्तता । मैं सिर्फ इन तीन की बात कर रहा हूं । ऐसे और भी कई अभागे होंगे । लेकिन इनकी बात इसलिये कर रहा हूं क्योंकि वे विज्ञानों अथवा आलोचना की पैदाईश थे ।”
आल्थुसर ने लिखा कि “जिस प्रकार मार्क्स ने ‘आर्थिक प्राणी’ (homo oeconomicus) के मिथक को ठुकरा कर अपने सिद्धांत की आधारशिला रखी उसी प्रकार फ्रायड ने ‘मनोवैज्ञानिक प्राणी’ (homopsychologicus) के मिथक को ठुकराया था । लकान ने फ्रायड के इस मुक्तिदायी स्फोट को देखा था । उसने उनके प्रत्येक शब्द को गंभीरता से लिया और उन्हें उनके तार्किक अंजाम तक पहुंचाया, बिना किसी दूसरी बात की परवाह किये । हो सकता है कि अन्य लोगों की तरह ही उन्होंने विस्तार में कुछ भूलें की हो, बल्कि उनके दार्शनिक निष्कर्षों का चयन भी सही न हो ; फ्रायड का विज्ञान एक नया विज्ञान था, मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के आविष्कार की तरह ही अवचेतन के आविष्कार से जुड़ा हुआ विज्ञान । मनोविश्लेषण को एक विज्ञान बताना स्वयं में बहुत बड़ी बात थी और इस मामले में यह भी सच है कि फ्रायड को खुद ही अपने इस विज्ञान का जनक बनना पड़ा था । उनके पहले इस क्षेत्र में वहां जो था, उसे अटकलबाजी और एक प्रकार का अंध-अन्वेषण भर कहा जा सकता है ।
(In the history of Western Reason, every care, foresight, precaution and warning has been devoted to births. Pre-natal therapy is institutional. When a young science is born, the family circle is always ready for astonishment, jubilation and baptism. For a long time, every child, even the foundling, has been reputed the son of a father, and when it is a prodigy, the fathers would fight at the gate if it were not for the mother and the respect due to her. In our crowded world, a place is allocated for birth, a place is even allocated for the prediction of a birth: ‘prospective’. To my knowledge, the 19th century saw the birth of two or three children that were not expected: Marx, Nietzsche and Freud. ‘Natural’ children, in the sense Freud and Lacan that nature offends customs, principles, morality and good breeding: nature is the rule violated, the unmarried mother, hence the absence of a legal father. Western Reason makes a fatherless child pay heavily. Marx, Nietzsche and Freud had to foot the often terrible bill of survival: a price compounded of exclusion, condemnation, insult, poverty, hunger and death, or madness. I speak only of them (other unfortunates might be mentioned who lived their death sentences in colour, sound and poetry). I speak only of them because they were the births of sciences or of criticism. That Freud knew poverty, calumny and persecution, that his spirit was well enough anchored to withstand, and interpret, all the insults of the age—these things may have something to do with certain of the limits and dead-ends of his genius. An examination of this point is probably premature. Let us instead consider Freud’s solitude in his own times. I do not mean human solitude (he had teachers and friends, though he went hungry), I mean theoretical solitude. For when he wanted to think i.e., to express in the form of a rigorous system of abstract concepts the extraordinary discovery that met him every day in his practice, search as he might for theoretical precedents, fathers in theory, he could find none. He had to cope with the following situation: to be himself his own father, to construct with his own craftsman’s hands the theoretical space in which to situate his discovery, to weave with thread borrowed intuitively left and right the great net with which to catch in the depths of blind experience the teeming fish of the unconscious, which men call dumb because it speaks even while they sleep.)
पश्चिम में भारतीय तंत्र शास्त्र की तरह मानव मन की गति-प्रकृति को साधने की कोई अलग से दीर्घकालीन पर्यवेक्षणमूलक परंपरा भी नहीं मिलती है । भारत में भी इस परंपरा को बहुत बाद में, खास तौर पर अभिनवगुप्त के माध्यम से ही बाकायदा एक सुसंगत शास्त्र का रूप मिल पाया था । अभिनवगुप्त ने शैवमत के तहत हजारों सालों के तांत्रिक उपक्रमों के बीच रचे गये लगभग 92 शैवागमों को समेटते हुए अपने 'तंत्रालोक' के जरिये इसे भारतीय दर्शनशास्त्र के इतिहास का एक सर्वाधिक विकसित और सुसंगत रूप दिया था । लेकिन आधुनिक काल में उस सूत्र को पकड़ कर हमारे यहां कोई सम्यक काम नहीं हुआ । उल्टे दर्शन के नैगमिक ग्रंथों को, वैदिक परंपरा को ही भारतीय दर्शनशास्त्र की मुख्यधारा के रूप में पीटा जाता रहा । इसकी तुलना में, पश्चिम में फ्रायड ने अपने ही कुशल हाथों से मनोजगत की गति की वह नई सैद्धांतिक जमीन तैयार की जिसपर वे इससे संबद्ध अपनी खोजों को स्थापित कर पाए थे । किसी बुनकर की तरह अपने ताने-बाने से क्रमशः उन्होंने उस जाल को बुना था जो अनुभूति के गहरे अंधेरे तल में जाकर अवचेतन की मछली को पकड़ कर ऊपर ला सके । वे मनुष्य के उस अवचेतन को प्रत्यक्ष करने में सफल हुए थे जिसे मनुष्य तब तक गूंगा मानता है, क्योंकि वह सिर्फ उसी समय बोलता है जब आदमी नींद में होता है, स्वप्न में होता है । शैव दर्शन की भाषा में जिसे हम एक परा-संसार भी कह सकते हैं ।
शैवमत के तंत्र शास्त्र से फ्रायड, लकान का बुनियादी फर्क तंत्र के आत्मवाद के अलावा के यह भी है कि फ्रायड के पास अपने इस काम के लिये आधुनिक विज्ञान की दूसरी सभी शाखाओं के सैद्धांतिक उपकरणों का प्रयोग करना संभव था । इसीलिये तंत्र के त्रिक दर्शन ने जो दूरियां हजारों साल के अपने पर्यवेक्षणों के कुल-क्रम के संकलन से तय की, उसे तय करके उन्हें ही हजारों साल पीछे छोड़ देने में फ्रायड और लकान को महज अपनी एक-एक जिंदगियां ही लगानी पड़ी । यह वास्तव में इस युग का करिश्मा है जब दो सौ साल पहले तक सदियों में पूरा होने वाले काम अब घंटों और मिनटों में होने लगे हैं ।
(क्रमशः)

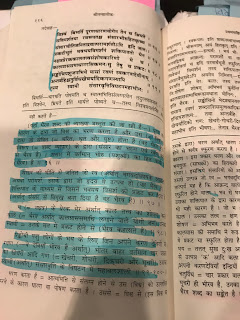



कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें