नोटबंदी के काले दिन की सालगिरह के मौके पर कोलकाता में लहक संगोष्ठी में पेश की गई विचार की एक प्रस्तावना :
—अरुण माहेश्वरी
आज 8 नवंबर । साल भर पहले हम अपने देश में एक ऐसे दृश्य के साक्षी हुए थे, जो हम सब, आजादी के बाद की पीढ़ी के लोगों की स्मृतियों में, एक अजीब प्रकार की डर और आश्चर्य मिश्रित अनुभूति पैदा करने वाले दृश्य की तरह शायद हमेशा रह जायेगी । अजीब इसलिये कि ऊपरी तौर पर तो इसमें एक भारी राष्ट्र-व्यापी उथल-पुथल की तरह की आपात स्थिति जैसी भागम-भाग की परिस्थिति दिखाई दे रही थी, लेकिन आश्चर्य इसलिये कि जो ऊपर से इतना तनावपूर्ण, मूलगामी और बड़ी चीज दिखाई दे रहा था, अंदर से वह उतना ही अधिक खोखला, निरर्थक और परिहासमूलक पाया गया और अन्ततः अब एक अबूझ सी पहेली बन कर रह गया ।
8 नवंबर की रात आठ बजे नोटबंदी की घोषणा के वक्त भारी तुमार बांधते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने अपने ऐलान के शुरू में ही कहा था कि आज से आपकी जेब में पड़ा 500 और 1000 रुपये का नोट मिट्टी हो गया, लेकिन जब दूसरे ही क्षण वे किसी सरकारी अधिकारी की तरह विस्तार से लोगों को यह बताने लगे थे कि कैसे वे दो दिन बाद बैंकों के सामने कतार में लग कर अपने पास पड़े हुए नोट को बदली करा सकते हैं, तभी विषय के जानकार हर व्यक्ति को उनकी घोषणा के पीछे के बेहूदापन को समझते और जोर से हंसते देर नहीं लगी थी । यह साफ हो गया था कि यह नोटबंदी नहीं, यह तो शुद्ध नोट-बदली है । सरकार पुराने नोटों की जगह लोगों को नये नोट देने जा रही है । और उसी समय हमने यह देख लिया था कि इसका कुल जमा परिणाम सिर्फ यह होगा कि देश का सारा कामकाज, कारोबार ठप हो जायेगा, करोड़ों लोग बैंकों के सामने दो महीनों तक कतारों में खड़े रहेंगे, बैंकों के भ्रष्ट अधिकारियों को नये नोटों के जरिये भारी कमाई का साधन मिलेगा और कई महीनों तक ऐसा लगेगा कि देश का हर आदमी सिर्फ एक ही काम और बात में लगा हुआ है कि अपने घर-दफ्तर में पड़े पुराने नोटों को जल्द से जल्द बदला कर कैसे वापस पाया जाए । और इन सबके बीच मदारी की तरह हंसते हुए हमारे प्रधानमंत्री यह कहते दिखाई देंगे कि 'देखा बच्चू ! क्या छकाया है तुम सबको । सब लोग हमारे इशारों पर इसी प्रकार नाचते रहने का अभ्यास कर लो । लोक व्यवहार में ऐसा अभ्यास — अर्थात एक मात्र हमारा स्वीकरण और अपर सबका पूर्ण तिरस्कार !
सरकार की शुरूआती घोषणाओं से ही यह भी साफ हो गया था कि सरकार ने पूरी तैयारी करके यह कदम नहीं उठाया है । उसके पास पुराने नोटों को नये में बदलने जितने नये नोट ही नहीं है और नये नोटों को छापने में उसे आगे कई महीने लगने वाले हैं ; अर्थात साधारण लोगों को अपनी अर्जित जमा पूंजी को बैंक में जमा करके वापस हासिल करने के लिये लंबा इंतजार और भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा । बिल्कुल वैसा ही हुआ भी ।
बैंकों के सामने कतारों में सौ से ज्यादा लोग मारे गये, हजारों कारखाने बंद हो गये, किसानों की नगद फसलों का कोई खरीदार नहीं रहा, बुवाई के काम के लिये खाद और बीज की खरीद जितने पैसे भी किसानों के पास नहीं रहे, बीमारी में इलाज का साधन तक नहीं बचा था । कुल मिला कर, देश की व्यापकतम जनता को एकाएक पूरी तरह से कंगाल हो जाने का गहरा धक्का लगा था । इससे आम लोगों में कोई आक्रोश न पैदा होने पाए, इसीलिये पूरे विषय को दूसरी दिशा में मोड़ने के लिये काला धन, आतंकवाद और जाली नोटों के विषय को सरकार की ओर से बहुत जोर-शोर के साथ प्रचारित किया जाने लगा । 'बड़े लोगों' के प्रति आम लोगों में ईर्ष्या के भाव के जरिये उनकी वंचना की अनुभूति को कम करने की कोशिश की जाने लगी ।
नोटबंदी के चंद रोज बाद ही जब दो हजार के जाली नोट और कश्मीर में आतंकवादियों के पास से नये नोट जब्त किये जाने लगे, तभी इसके साथ जाली नोट और आतंकवाद का जो आख्यान तैयार किया गया है, उसके झूठ का पर्दाफाश हो गया था । खुद सरकार के संस्थान आईएसआई के आंकड़े कह रहे थे कि भारत में चल रहे जाली नोटों की मात्रा प्रचलन की कुल मुद्रा के 0.025 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है ।
उस दौर में एक समय प्रधानमंत्री के साथ ही नीति आयोग और वित्त मंत्रालय की ओर से यह कहा जाने लगा था कि नोटबंदी के अंत में कम से कम 2 से 3 लाख करोड़ रुपये ऐसे रह जायेंगे जिन्हें जमा कराने कोई नहीं आयेगा और यह रिजर्व बैंक की एक अतिरिक्त आमदनी होगी । उन्हीं दिनों हमने इस धोखे पर से पर्दा उठाते हुए लिखा था सबसे अधिक संभावना इस बात की है कि 500 और 1000 रुपये के जितने, 15 लाख करोड़ की राशि के नोट चलन में हैं, उनसे कम नहीं बल्कि ज्यादा ही रुपये बैंकों में जमा होने की संभावना है । हमने मोदी के काम करने के ढंग की आलोचना करते हुए बताया था कि यदि सरकार ने सिर्फ अपने ही विभाग, सीबीडीटी से संपर्क करके यह पता लगा लिया होता कि तमाम कंपनियों के पास 'कैस इन हैंड' में कितनी राशि पड़ी हुई है तो उसे पता चल जाता कि बाजार में जितनी नगद राशि चलन में नहीं है, उससे काफी ज्यादा कंपनियों के खातों में नगद के रूप में पड़ी हुई है।
मोदी के ऐसे तमाम बेबुनियाद दावों की जब पोल खुलने लगी तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने यह कदम नगदी में लेन-देन को खत्म करके डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिये उठाया है । उसी समये हमारे सामने साफ था कि नोटबंदी के उन दिनों में जब बाजार में नगदी की भारी कमी हो गई थी, तब भले ही मजबूरीवश लोग अपनी मूलभूत जरूरतों के लिये बैंक खातों और कार्डों का अपेक्षाकृत ज्यादा प्रयोग कर लें, लेकिन जैसे ही बाजार में धीरे-धीरे नगदी की सहूलियत होगी, लोग पहले की तुलना में कहीं ज्यादा नगद लेन-देन का रास्ता अपनायेंगे । इसकी वजह यह है कि नोटबंदी के इस कष्टदायी अनुभव से लोगों का बैंकों के प्रति विश्वास ही डोल चुका था । हम समझ रहे थे कि आगे से लोग अपने पास ज्यादा से ज्यादा नगदी रखना ही पसंद करेंगे ताकि जीवन में आने वाली सभी आपद-विपद के समय उनके खुद के पास खर्च के लायक राशि मौजूद रहे । और तभी यह भी साफ हो गया था कि नोटबंदी भारतीय अर्थ-व्यवस्था को एक ऐसी मंदी में धकेल देगी, जिससे उबर पाना उसके लिये एक टेढ़ी खीर साबित होगी ।
राज्य सभा में मनमोहन सिंह ने इन सभी बातों को संक्षिप्त रूप में रखते हुए सही कहा था कि यह भारत की जनता की आमदनी की एक खुली लूट है और इसके चलते भारत के जीडीपी में कम से कम दो प्रतिशत की गिरावट आएगी ।
नोटबंदी के बाद के इस एक साल में ये सभी बातें सौ प्रतिशत सही साबित हुई है । जिस रिजर्व बैंक की अतिरिक्त आमदनी के सपने दिखाये गये थे, उसे उल्टे 30 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है । कुल मिला कर, दुनिया की सबसे तेज गति से विकसित हो रही भारत की अर्थ-व्यवस्था को मोदी ने अपनी सनक में एक बार के लिये पूरी तरह से पटरी से उतार दिया । हाल में ईपीडब्लू में किये गये एक अध्ययन से पता चलता है कि सत्तर साल के आजाद भारत में पहली बार भारत में रोजगारों में वृद्धि के बजाय कमी आई है । नोटबंदी के समय असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर काम बंद हो जाने के कारण गांव लौट गये थे, उनमें से एक अच्छा-खासा हिस्सा इतना हताश हो गया है कि वापस काम की तलाश में वह शहर में लौटा ही नहीं है। पहले हम जहां भारत की युवा आबादी पर गर्व करते हुए कहते थे कि यह श्रम शक्ति सारी दुनिया में भारत को एक पहली पंक्ति के देश में बदल देगी, वही भारत आज दुनिया में काम न चाहने वाले समर्थ लोगों की सबसे बड़ी आबादी का देश बन गया है । यहां की श्रम शक्ति का लगभग 54 प्रतिशत हिस्सा हताशावश अपने को श्रम के बाजार से ही अलग कर चुका है !
जब आदमी में आमदनी के प्रति ही विरक्ति का भाव बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से उसका पूरी अर्थ-व्यवस्था पर मंदी के रूप में कितना नकारात्मक असर पड़ता है, आज भारतीय अर्थ-व्यवस्था उसी मंदी में फंस चुकी है । अर्थशास्त्री हमेशा कहते हैं कि मंदी का एक प्रमुख कारण आम उपभोक्ता के मनोविज्ञान से जुड़ा होता है । खुश और निश्चिंत आदमी अपनी क्षमता से भी ज्यादा खर्च करने से नहीं घबड़ाता, जबकि परेशान और आमदनी के बारे में अनिश्चयता का शिकार आदमी अपनी न्यूनतम जरूरतों में भी कटौती करके विपत्ति के समय के लिये धन जुटाने में लगा रहता है । आज आम लोगों की यही मनोदशा है । सब थोड़े में गुजर करने की पूर्वजों की शिक्षा पर अमल कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि भारत का आंतरिक बाजार सिकुड़ता जा रहा है ।
बहरहाल, ये तमाम ऐसी बातें हैं, जिन्हें हम सभी अपने निजी अनुभवों से और देश-दुनिया की जानकारी के आधार पर भी जानते-समझते हैं । इसके खिलाफ आज देश के हर कोने से आवाजें उठ रही है और मीडिया आदि के जरिये वर्तमान सरकार अपने सीने को कितना भी अधिक चौड़ा दिखाने की कोशिश क्यों न करे, क्रमशः आज स्थिति यह है कि गुजरात की तरह के अपने सबसे मजबूत गढ़ में भी मोदी के लिये अपनी जीत को कायम रखना एक भारी चुनौती का रूप ले चुका है, अन्य जगहों की बात तो जाने ही दीजिए ।
इसी बीच हड़बड़ी और राजनीतिक संकीर्ण स्वार्थों के लिये ही पुनः जीएसटी के कदम ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है । यह एक और प्रसंग है, जिस पर फिर अलग से चर्चा हो सकती है । 30 जून की रात बारह बजे संसद के संयुक्त सदन के जरिये जिस नाटकीय अंदाज में इसे लागू किया गया, उसकी यह कितनी बड़ी ट्रैजेडी है कि आज वही प्रधानमंत्री गुजरात के लोगों से यह कहते हुए क्षमा मांग रहा है कि जीएसटी के लिये अकेले उन्हें अपराधी के कठघरे में खड़ा न किया जाए ! इसके पीछे मूलतः कांग्रेस का हाथ रहा है !
जो भी हो, इस भयानक अनुभव के साल भर बाद, बुद्धजीवी कहलाने के नाते हमारे सामने कुछ और सवाल भी है । आम जीवन के इन अपने प्रकार के बेहद डरावने अनुभवों से गुजरने के बाद भी क्या हम बुद्धिजीवी के नाते, इस भयानक सचाई के अन्तरनिहित तात्विक सच को पकड़ पा रहे हैं ? क्या हम अपने आज के समय के पूरे संदर्भ में इसकी सही व्याख्या कर पा रहे हैं ताकि हम इस प्रकार के स्वेच्छाचारी कदमों के अंदर की उन दरारों पर रोशनी डाल सके जिनसे हम न सिर्फ अपनी जनतांत्रिक व्यवस्था के नैतिक, न्यायिक और राजनीतिक आधार की तात्विक कमजोरी को पहचान पाए, बल्कि हमारे यहां फासीवाद के विरोध के विमर्श की जो अब तक जो अपनी कमजोरियां सामने आती रही हैं, उन्हें भी एक हद तक देख पाएं । फासीवाद क्या है, मोदी और आरएसएस फासीवादी हैं, या नहीं — इस प्रकार के सवाल आज भी खास तौर पर वामपंथ के दायरे में अभी भी गाहे-बगाहे उठते रहते हैं ।
आम तौर पर वामपंथियों के बीच फासीवाद के बारे में, चालीस के जमाने से ही यह एक शास्त्रीय परिभाषा प्रचलित है कि यह वित्तीय पूंजी के सबसे निकृष्ट रूप की एक अभिव्यक्ति है । अर्थात, पूंजीवाद तो हमारे यहां एक मान्य सत्य है ही, जब हम फासीवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं तब हम सिर्फ उस क्षण को टालने के लिये लड़ रहे होते हैं जब यह पूंजीवाद अपने सबसे निकृष्ट रूप में सामने आता है । और यही वह समझ है जो खास तौर पर बुद्धिजीवियों के एक अच्छे-खासे हिस्से के सोच में एक ऐसा गतिरोध पैदा कर देती है कि उसे इस पूरी लड़ाई के महत्व के सार पर ही संदेह होने लगता है और उल्टे वह फासीवादी सत्ता के साथ ही सुलह करके रहने में कोई बुराई महसूस नहीं करता है । हिटलर के जमाने में जर्मनी के सबसे बड़े दार्शनिक हाइडेगर ने नाजीवाद के बारे में अपनी तात्विक समझ की इसी बिनाह पर हिटलर के साथ निबाह करके चलने के अपने रास्ते की पैरवी की थी । जब कोई इस प्रकार की उलझन में फंस जाता है तब उसके सामने आगे चलने का कोई निर्विकल्प रास्ता शेष नहीं रह जाता है, सब कुछ गड्ड-मड्ड दिखाई देने लगता है । खास तौर पर वामपंथियों के एक अच्छे खासे तबके में इससे ऐसी भारी उलझने पैदा होने लगती हैं जिसके कारण फासीवाद के खिलाफ व्यापकतम एकता के साथ समझौताहीन संघर्ष के लिये जरूरी रणनीति से वह इन नाना तात्विक उलझनों के चलते कई प्रकार से समझौते करने लगता है । वह जनतांत्रिक ताकतों की वर्गीय पहचान के नाम पर उन सबकी एकजुट लड़ाई के प्रति संशयग्रस्त हो जाता है ।
कहना न होगा, वामपंथी खेमे की इन उलझनों के मूल में पूंजीवादी जनतंत्र, जिसमें मानव अधिकारों की कद्र की जाती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मान किया जाता है, कानून का शासन होता है जिसके सामने सब समान होते हैं, और फासीवाद, जिसमें मानव अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोट दिया जाता है, कानून के शासन के बजाय एक तानाशाह के हुक्म चला करते हैं — इन दोनों को एक पूंजीवाद के ही दो रूप मान लेने की मूलभूत रूप से एक गलत विचारधारात्मक समझ काम कर रही होती है ।
यहां हमारी विचार की प्रस्तावना का मूल विषय यही है कि जब तक हम पूंजीवाद, फासीवाद और समाजवाद — इन तीनों को एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न, अलग-अलग स्वायत्त समाज-व्यवस्थाओं के रूप में नहीं देखेंगे, हम कभी भी फासीवाद के खिलाफ संघर्ष की सही दिशा में सोच-विचार नहीं कर पायेंगे ।
मार्क्स ने कहा था कि उत्पादन का स्वरूप ही किसी भी समाज में आदमी के जीवन का स्वरूप होता है । इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया था कि उत्पादन के साधनों की मिल्कियत अर्थात उत्पादन-संबंध किसी भी समाज के सामाजिक संबंधों, सामाजिक-व्यवस्था को व्यक्त करते हैं । जब हम उत्पादन के स्वरूप के आधार पर ही समाज व्यवस्थाओं पर राय देने लगते हैं तब हम वही भूल करने के लिये मजबूर हो जायेंगे जो भूल हर्बर्ट मारक्यूस से लेकर फ्रैंकफर्ट स्कूल कहे जाने वाले दार्शनिकों ने साठ के दशक में पूंजीवाद और समाजवाद, दोनों को एक ही आधुनिक तकनीक के औद्योगिक युग की समाज-व्यवस्था मान कर, दोनों को समान बता देने की भूल की थी । उन्होंने उत्पादन के साधनों के सामाजीकरण के उस सच की अवहेलना की थी जो समाजवाद को पूंजीवाद से मूलभूत रूप में अलग करता है ।
यही बात फासीवाद के बारे में भी समान रूप से लागू होती है । थोड़ी सी गहराई में जाने से ही हम देख पायेंगे कि फासीवाद उत्पादन संबंधों के उस रूप पर टिका हुआ है जिसमें उत्पादन के साधनों की निजी मिल्कियत के बावजूद उनका तानाशाही शासन की कमांड व्यवस्था से संचालन किया जाता है । हिटलर ने ट्रेडयूनियन आंदोलन को कुचल कर पूंजीपतियों को मजदूरों की सौदेबाजी के दबाव से मुक्त कर दिया, लेकिन इसके साथ ही खुद पूंजीपतियों के लिये भी यह तय कर दिया कि जर्मनी के कारखानों में किस चीज का कितना उत्पादन किया जायेगा; किस प्रकार वे विश्व विजय की हिटलर की योजना की सेवा में लगे रहेंगे । अर्थात, उद्योग चलेंगे पूरी तरह से हिटलर के फरमानों के अनुसार । जैसे भारत में मोदी ने पूरी अर्थ-व्यवस्था को अपनी निजी मुट्ठी में कस लेने के लिये नोटबंदी की तरह का सामान्य रूप से निंदित कदम उठाने में जरा सी भी हिचक का परिचय नहीं दिया । अर्थ-व्यवस्था के सामान्य मान्य नियमों को ताक पर रख कर उसे एक तानाशाह की सनक के अधीन कर देने की यही लाक्षणिकता मोदी और आरएसएस के फासीवादी चरित्र का एक सबसे बड़ा सबूत पेश करती है । हिटलर ने अपने काल में उन सभी उद्योगपतियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था जिन्होंने हिटलर के उदय में उसकी सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता की थी । (देखें, अरुण माहेश्वरी : हिटलर और व्यवसायी वर्ग https://chaturdik.blogspot.in/2016/03/blog-post_10.html)
इसकी तुलना में सामान्य पूंजीवादी जनतंत्र मूलतः उत्पादन के साधनों की निजि मिल्कियत पर टिका होने पर भी वह किसी कमांड व्यवस्था के जरिये नहीं, बल्कि मूलतः बाजार के नियमों से संचालित होता है, जिसमें पूंजी के मूलभूत अधिकार को स्वीकृति के साथ ही सामान्य उपभोक्ता समाज की एक सक्रिय भागीदारी भी हुआ करती है । उपभोक्ता के हितों की रक्षा भी राज्य का एक प्रमुख दायित्व होता है । नागरिक के अधिकार, मानव-अधिकार, कानून का शासन की संगति में ही पूंजीपति और उपभोक्ता के अधिकार भी अपनी न्यायोचितता को प्रमाणित करते हैं ।
इस प्रकार, आधुनिक तकनीक के औद्योगिक युग के एक ही क्षितिज में उभर कर आने वाली इन तीन अलग-अलग समाज-व्यवस्थाओं, पूंजीवादी जनतंत्र, फासीवाद और समाजवाद को हम तात्विक रूप में बिल्कुल तीन अलग-अलग जगहों पर रख कर स्वतंत्र रूप में समझ सकते हैं और इन तीनों व्यवस्थाओं के तहत सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक मान-मूल्यों को भी अलग—अलग करके देखा जा सकता है।
यही वह संदर्भ है जिससे पता चलता है कि जहां से पूंजीवादी जनतंत्र का संकट यदि फासीवाद के आगमन का कारण बन सकता है, वहीं से समाजवाद के द्वार भी खोल सकता है । मूल प्रश्न मनुष्य द्वारा पहले से उपार्जित शक्तियों और अधिकारों की रक्षा से जुड़ा होता है । यह समय और स्थान के एक वृत्त से मुक्त होकर बिल्कुल दूसरे वृत्त में प्रवेश की तरह है । नवंबर क्रांति की विद्रोही विरासत तबाह की जा रही उच्छिष्ट मानव-शक्ति को सामाजिक रूपांतरण की एक नई संगठित, सृजनात्मक शक्ति में बदलने का संदेश देती है। हर समाज में बनने वाले द्वंद्वात्मक संयोगों को मानव-मुक्तिकारी समाज व्यवस्थाओं में उतारना ही क्रांतिकारियों का काम है।जीवन के सभी स्तरों पर मार्क्सवाद के प्रयोग की स्थितियों को समझते हुए उन्हें मूर्त करने में ही यह क्रांतिकारी विज्ञान चरितार्थ होता है।
और, जैसे ही हम समाज-व्यवस्थाओँ और उसमें होने वाले परिवर्तनों की इस प्रकार की एक स्पष्ट तात्विक समझ को हासिल करेंगे, हमें भारतीय राजनीति में पिछले लगभग सत्तर साल से शासन की नीतियों को तय कर रही कांग्रेस पार्टी और आज उसके नेता राहुल गांधी और हिटलर के नाजीवादी एकीकृत शासन की समझ पर चलने वाली आरएसएस और नोटबंदी तथा विकृत ढंग से जीएसटी लागू करने वाले तुगलकी नेता नरेन्द्र मोदी के बीच फर्क करने में कोई कठिनाई नहीं होगी । फासीवाद से लड़ाई को लेकर हमारे सामने तब कोई मानसिक गतिरोध नहीं होगा । हमें मोदी के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में ही व्यापकतम एकजुट आंदोलन की रणनीति से अपने को जोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी । हमारे देश में हमें अपने धर्म-निरपेक्ष और कल्याणकारी राज्य के संविधान की रक्षा की लड़ाई के जरिये पूरे समाज के हितार्थ मनुष्यों की अब तक अर्जित शक्तियों और उनके अधिकारों के प्रयोग को सुनिश्चित करना है। शोषण की ताकतें इस नई परिस्थिति का इस्तेमाल राज्य को अधिक से अधिक दमन-मूलक बनाने के लिये करेगी। हमारे जैसे देश में बेरोजगारों की बढ़ती हुई फौज को गुंडों-बदमाशों (गोगुंडों) की फौज में बदलने की कोशिश आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। इससे दंगाइयों की, अन्ध-राष्ट्रवाद के नशे में चूर आत्म-घाती युद्धबाजों की फौज बनाई जायेगी। लेकिन उतना ही बड़ा सच यह भी है कि यह हिटलर का, औद्योगिक पूंजीवाद के प्रथम चरण का जमाना नहीं है। यह मनुष्यों के आत्म-विखंडन से लेकर समान स्तर पर विखंडित, अकेले मनुष्यों की नई सामाजिकता का जमाना भी है। मूल बात यह है कि हवाई हो या ठोस, मनुष्यों द्वारा अर्जित नई उत्पादन शक्तियों के अनुरूप मानव समाज के नये स्वरूपों के निरूपण को कोई रोक नहीं सकता है। इसका प्रभाव मनुष्यों के सामाजिक जीवन पर जितना पड़ेगा, उससे कम चिंतन के स्तर पर तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा के स्तर तक नहीं पड़ेगा ।
आज जब हम नोटबंदी की तरह के एक चरम तुगलकी कदम से सामान्य जन-जीवन में मची हुई अफरा-तफरी की परिस्थितियों में नोटबंदी की घोषणा के काले दिन के एक साल पूरा होने के दिन की ओर बढ़ रहे हैं, हमें लगता है कि यह जरूरी है कि आधुनिक काल में समाज-व्यवस्थाओं के भिन्न-भिन्न रूपों की विविधताओं की तात्विकता के बारे में हमारी एक समझ बनें ताकि एक बुद्धिजीवी के नाते हम जिस विचारधारात्मक बिंदु पर अपने सामने उलझन की एक अवस्था देखते हैं, उस फांस से हम अपने को मुक्त कर सके, और बिना किसी संशय के अपने वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक दायित्वों का निर्वाह कर सके ।
नोटबंदी के बारे में हमारी यह किताब इस लिहाज से यदि जरा सी भी मददगार साबित हो सके तो हम उसे इसकी सफलता मानेंगे । नोटबंदी के उस दौर के जो चित्र आपको इस किताब में मिलेंगे, उनके ही आत्मिक प्रभावों को आप सरला की इस दौर की कविताओँ में देख पायेंगे, जिसका शीर्षक ही इसकी सारी कहानी को कह देता है — ये जिंदगी की मुर्दा कतारें ।
धन्यवाद ।
—अरुण माहेश्वरी
आज 8 नवंबर । साल भर पहले हम अपने देश में एक ऐसे दृश्य के साक्षी हुए थे, जो हम सब, आजादी के बाद की पीढ़ी के लोगों की स्मृतियों में, एक अजीब प्रकार की डर और आश्चर्य मिश्रित अनुभूति पैदा करने वाले दृश्य की तरह शायद हमेशा रह जायेगी । अजीब इसलिये कि ऊपरी तौर पर तो इसमें एक भारी राष्ट्र-व्यापी उथल-पुथल की तरह की आपात स्थिति जैसी भागम-भाग की परिस्थिति दिखाई दे रही थी, लेकिन आश्चर्य इसलिये कि जो ऊपर से इतना तनावपूर्ण, मूलगामी और बड़ी चीज दिखाई दे रहा था, अंदर से वह उतना ही अधिक खोखला, निरर्थक और परिहासमूलक पाया गया और अन्ततः अब एक अबूझ सी पहेली बन कर रह गया ।
8 नवंबर की रात आठ बजे नोटबंदी की घोषणा के वक्त भारी तुमार बांधते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने अपने ऐलान के शुरू में ही कहा था कि आज से आपकी जेब में पड़ा 500 और 1000 रुपये का नोट मिट्टी हो गया, लेकिन जब दूसरे ही क्षण वे किसी सरकारी अधिकारी की तरह विस्तार से लोगों को यह बताने लगे थे कि कैसे वे दो दिन बाद बैंकों के सामने कतार में लग कर अपने पास पड़े हुए नोट को बदली करा सकते हैं, तभी विषय के जानकार हर व्यक्ति को उनकी घोषणा के पीछे के बेहूदापन को समझते और जोर से हंसते देर नहीं लगी थी । यह साफ हो गया था कि यह नोटबंदी नहीं, यह तो शुद्ध नोट-बदली है । सरकार पुराने नोटों की जगह लोगों को नये नोट देने जा रही है । और उसी समय हमने यह देख लिया था कि इसका कुल जमा परिणाम सिर्फ यह होगा कि देश का सारा कामकाज, कारोबार ठप हो जायेगा, करोड़ों लोग बैंकों के सामने दो महीनों तक कतारों में खड़े रहेंगे, बैंकों के भ्रष्ट अधिकारियों को नये नोटों के जरिये भारी कमाई का साधन मिलेगा और कई महीनों तक ऐसा लगेगा कि देश का हर आदमी सिर्फ एक ही काम और बात में लगा हुआ है कि अपने घर-दफ्तर में पड़े पुराने नोटों को जल्द से जल्द बदला कर कैसे वापस पाया जाए । और इन सबके बीच मदारी की तरह हंसते हुए हमारे प्रधानमंत्री यह कहते दिखाई देंगे कि 'देखा बच्चू ! क्या छकाया है तुम सबको । सब लोग हमारे इशारों पर इसी प्रकार नाचते रहने का अभ्यास कर लो । लोक व्यवहार में ऐसा अभ्यास — अर्थात एक मात्र हमारा स्वीकरण और अपर सबका पूर्ण तिरस्कार !
सरकार की शुरूआती घोषणाओं से ही यह भी साफ हो गया था कि सरकार ने पूरी तैयारी करके यह कदम नहीं उठाया है । उसके पास पुराने नोटों को नये में बदलने जितने नये नोट ही नहीं है और नये नोटों को छापने में उसे आगे कई महीने लगने वाले हैं ; अर्थात साधारण लोगों को अपनी अर्जित जमा पूंजी को बैंक में जमा करके वापस हासिल करने के लिये लंबा इंतजार और भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा । बिल्कुल वैसा ही हुआ भी ।
बैंकों के सामने कतारों में सौ से ज्यादा लोग मारे गये, हजारों कारखाने बंद हो गये, किसानों की नगद फसलों का कोई खरीदार नहीं रहा, बुवाई के काम के लिये खाद और बीज की खरीद जितने पैसे भी किसानों के पास नहीं रहे, बीमारी में इलाज का साधन तक नहीं बचा था । कुल मिला कर, देश की व्यापकतम जनता को एकाएक पूरी तरह से कंगाल हो जाने का गहरा धक्का लगा था । इससे आम लोगों में कोई आक्रोश न पैदा होने पाए, इसीलिये पूरे विषय को दूसरी दिशा में मोड़ने के लिये काला धन, आतंकवाद और जाली नोटों के विषय को सरकार की ओर से बहुत जोर-शोर के साथ प्रचारित किया जाने लगा । 'बड़े लोगों' के प्रति आम लोगों में ईर्ष्या के भाव के जरिये उनकी वंचना की अनुभूति को कम करने की कोशिश की जाने लगी ।
नोटबंदी के चंद रोज बाद ही जब दो हजार के जाली नोट और कश्मीर में आतंकवादियों के पास से नये नोट जब्त किये जाने लगे, तभी इसके साथ जाली नोट और आतंकवाद का जो आख्यान तैयार किया गया है, उसके झूठ का पर्दाफाश हो गया था । खुद सरकार के संस्थान आईएसआई के आंकड़े कह रहे थे कि भारत में चल रहे जाली नोटों की मात्रा प्रचलन की कुल मुद्रा के 0.025 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है ।
उस दौर में एक समय प्रधानमंत्री के साथ ही नीति आयोग और वित्त मंत्रालय की ओर से यह कहा जाने लगा था कि नोटबंदी के अंत में कम से कम 2 से 3 लाख करोड़ रुपये ऐसे रह जायेंगे जिन्हें जमा कराने कोई नहीं आयेगा और यह रिजर्व बैंक की एक अतिरिक्त आमदनी होगी । उन्हीं दिनों हमने इस धोखे पर से पर्दा उठाते हुए लिखा था सबसे अधिक संभावना इस बात की है कि 500 और 1000 रुपये के जितने, 15 लाख करोड़ की राशि के नोट चलन में हैं, उनसे कम नहीं बल्कि ज्यादा ही रुपये बैंकों में जमा होने की संभावना है । हमने मोदी के काम करने के ढंग की आलोचना करते हुए बताया था कि यदि सरकार ने सिर्फ अपने ही विभाग, सीबीडीटी से संपर्क करके यह पता लगा लिया होता कि तमाम कंपनियों के पास 'कैस इन हैंड' में कितनी राशि पड़ी हुई है तो उसे पता चल जाता कि बाजार में जितनी नगद राशि चलन में नहीं है, उससे काफी ज्यादा कंपनियों के खातों में नगद के रूप में पड़ी हुई है।
मोदी के ऐसे तमाम बेबुनियाद दावों की जब पोल खुलने लगी तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने यह कदम नगदी में लेन-देन को खत्म करके डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिये उठाया है । उसी समये हमारे सामने साफ था कि नोटबंदी के उन दिनों में जब बाजार में नगदी की भारी कमी हो गई थी, तब भले ही मजबूरीवश लोग अपनी मूलभूत जरूरतों के लिये बैंक खातों और कार्डों का अपेक्षाकृत ज्यादा प्रयोग कर लें, लेकिन जैसे ही बाजार में धीरे-धीरे नगदी की सहूलियत होगी, लोग पहले की तुलना में कहीं ज्यादा नगद लेन-देन का रास्ता अपनायेंगे । इसकी वजह यह है कि नोटबंदी के इस कष्टदायी अनुभव से लोगों का बैंकों के प्रति विश्वास ही डोल चुका था । हम समझ रहे थे कि आगे से लोग अपने पास ज्यादा से ज्यादा नगदी रखना ही पसंद करेंगे ताकि जीवन में आने वाली सभी आपद-विपद के समय उनके खुद के पास खर्च के लायक राशि मौजूद रहे । और तभी यह भी साफ हो गया था कि नोटबंदी भारतीय अर्थ-व्यवस्था को एक ऐसी मंदी में धकेल देगी, जिससे उबर पाना उसके लिये एक टेढ़ी खीर साबित होगी ।
राज्य सभा में मनमोहन सिंह ने इन सभी बातों को संक्षिप्त रूप में रखते हुए सही कहा था कि यह भारत की जनता की आमदनी की एक खुली लूट है और इसके चलते भारत के जीडीपी में कम से कम दो प्रतिशत की गिरावट आएगी ।
नोटबंदी के बाद के इस एक साल में ये सभी बातें सौ प्रतिशत सही साबित हुई है । जिस रिजर्व बैंक की अतिरिक्त आमदनी के सपने दिखाये गये थे, उसे उल्टे 30 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है । कुल मिला कर, दुनिया की सबसे तेज गति से विकसित हो रही भारत की अर्थ-व्यवस्था को मोदी ने अपनी सनक में एक बार के लिये पूरी तरह से पटरी से उतार दिया । हाल में ईपीडब्लू में किये गये एक अध्ययन से पता चलता है कि सत्तर साल के आजाद भारत में पहली बार भारत में रोजगारों में वृद्धि के बजाय कमी आई है । नोटबंदी के समय असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर काम बंद हो जाने के कारण गांव लौट गये थे, उनमें से एक अच्छा-खासा हिस्सा इतना हताश हो गया है कि वापस काम की तलाश में वह शहर में लौटा ही नहीं है। पहले हम जहां भारत की युवा आबादी पर गर्व करते हुए कहते थे कि यह श्रम शक्ति सारी दुनिया में भारत को एक पहली पंक्ति के देश में बदल देगी, वही भारत आज दुनिया में काम न चाहने वाले समर्थ लोगों की सबसे बड़ी आबादी का देश बन गया है । यहां की श्रम शक्ति का लगभग 54 प्रतिशत हिस्सा हताशावश अपने को श्रम के बाजार से ही अलग कर चुका है !
जब आदमी में आमदनी के प्रति ही विरक्ति का भाव बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से उसका पूरी अर्थ-व्यवस्था पर मंदी के रूप में कितना नकारात्मक असर पड़ता है, आज भारतीय अर्थ-व्यवस्था उसी मंदी में फंस चुकी है । अर्थशास्त्री हमेशा कहते हैं कि मंदी का एक प्रमुख कारण आम उपभोक्ता के मनोविज्ञान से जुड़ा होता है । खुश और निश्चिंत आदमी अपनी क्षमता से भी ज्यादा खर्च करने से नहीं घबड़ाता, जबकि परेशान और आमदनी के बारे में अनिश्चयता का शिकार आदमी अपनी न्यूनतम जरूरतों में भी कटौती करके विपत्ति के समय के लिये धन जुटाने में लगा रहता है । आज आम लोगों की यही मनोदशा है । सब थोड़े में गुजर करने की पूर्वजों की शिक्षा पर अमल कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि भारत का आंतरिक बाजार सिकुड़ता जा रहा है ।
बहरहाल, ये तमाम ऐसी बातें हैं, जिन्हें हम सभी अपने निजी अनुभवों से और देश-दुनिया की जानकारी के आधार पर भी जानते-समझते हैं । इसके खिलाफ आज देश के हर कोने से आवाजें उठ रही है और मीडिया आदि के जरिये वर्तमान सरकार अपने सीने को कितना भी अधिक चौड़ा दिखाने की कोशिश क्यों न करे, क्रमशः आज स्थिति यह है कि गुजरात की तरह के अपने सबसे मजबूत गढ़ में भी मोदी के लिये अपनी जीत को कायम रखना एक भारी चुनौती का रूप ले चुका है, अन्य जगहों की बात तो जाने ही दीजिए ।
इसी बीच हड़बड़ी और राजनीतिक संकीर्ण स्वार्थों के लिये ही पुनः जीएसटी के कदम ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है । यह एक और प्रसंग है, जिस पर फिर अलग से चर्चा हो सकती है । 30 जून की रात बारह बजे संसद के संयुक्त सदन के जरिये जिस नाटकीय अंदाज में इसे लागू किया गया, उसकी यह कितनी बड़ी ट्रैजेडी है कि आज वही प्रधानमंत्री गुजरात के लोगों से यह कहते हुए क्षमा मांग रहा है कि जीएसटी के लिये अकेले उन्हें अपराधी के कठघरे में खड़ा न किया जाए ! इसके पीछे मूलतः कांग्रेस का हाथ रहा है !
जो भी हो, इस भयानक अनुभव के साल भर बाद, बुद्धजीवी कहलाने के नाते हमारे सामने कुछ और सवाल भी है । आम जीवन के इन अपने प्रकार के बेहद डरावने अनुभवों से गुजरने के बाद भी क्या हम बुद्धिजीवी के नाते, इस भयानक सचाई के अन्तरनिहित तात्विक सच को पकड़ पा रहे हैं ? क्या हम अपने आज के समय के पूरे संदर्भ में इसकी सही व्याख्या कर पा रहे हैं ताकि हम इस प्रकार के स्वेच्छाचारी कदमों के अंदर की उन दरारों पर रोशनी डाल सके जिनसे हम न सिर्फ अपनी जनतांत्रिक व्यवस्था के नैतिक, न्यायिक और राजनीतिक आधार की तात्विक कमजोरी को पहचान पाए, बल्कि हमारे यहां फासीवाद के विरोध के विमर्श की जो अब तक जो अपनी कमजोरियां सामने आती रही हैं, उन्हें भी एक हद तक देख पाएं । फासीवाद क्या है, मोदी और आरएसएस फासीवादी हैं, या नहीं — इस प्रकार के सवाल आज भी खास तौर पर वामपंथ के दायरे में अभी भी गाहे-बगाहे उठते रहते हैं ।
आम तौर पर वामपंथियों के बीच फासीवाद के बारे में, चालीस के जमाने से ही यह एक शास्त्रीय परिभाषा प्रचलित है कि यह वित्तीय पूंजी के सबसे निकृष्ट रूप की एक अभिव्यक्ति है । अर्थात, पूंजीवाद तो हमारे यहां एक मान्य सत्य है ही, जब हम फासीवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं तब हम सिर्फ उस क्षण को टालने के लिये लड़ रहे होते हैं जब यह पूंजीवाद अपने सबसे निकृष्ट रूप में सामने आता है । और यही वह समझ है जो खास तौर पर बुद्धिजीवियों के एक अच्छे-खासे हिस्से के सोच में एक ऐसा गतिरोध पैदा कर देती है कि उसे इस पूरी लड़ाई के महत्व के सार पर ही संदेह होने लगता है और उल्टे वह फासीवादी सत्ता के साथ ही सुलह करके रहने में कोई बुराई महसूस नहीं करता है । हिटलर के जमाने में जर्मनी के सबसे बड़े दार्शनिक हाइडेगर ने नाजीवाद के बारे में अपनी तात्विक समझ की इसी बिनाह पर हिटलर के साथ निबाह करके चलने के अपने रास्ते की पैरवी की थी । जब कोई इस प्रकार की उलझन में फंस जाता है तब उसके सामने आगे चलने का कोई निर्विकल्प रास्ता शेष नहीं रह जाता है, सब कुछ गड्ड-मड्ड दिखाई देने लगता है । खास तौर पर वामपंथियों के एक अच्छे खासे तबके में इससे ऐसी भारी उलझने पैदा होने लगती हैं जिसके कारण फासीवाद के खिलाफ व्यापकतम एकता के साथ समझौताहीन संघर्ष के लिये जरूरी रणनीति से वह इन नाना तात्विक उलझनों के चलते कई प्रकार से समझौते करने लगता है । वह जनतांत्रिक ताकतों की वर्गीय पहचान के नाम पर उन सबकी एकजुट लड़ाई के प्रति संशयग्रस्त हो जाता है ।
कहना न होगा, वामपंथी खेमे की इन उलझनों के मूल में पूंजीवादी जनतंत्र, जिसमें मानव अधिकारों की कद्र की जाती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मान किया जाता है, कानून का शासन होता है जिसके सामने सब समान होते हैं, और फासीवाद, जिसमें मानव अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोट दिया जाता है, कानून के शासन के बजाय एक तानाशाह के हुक्म चला करते हैं — इन दोनों को एक पूंजीवाद के ही दो रूप मान लेने की मूलभूत रूप से एक गलत विचारधारात्मक समझ काम कर रही होती है ।
यहां हमारी विचार की प्रस्तावना का मूल विषय यही है कि जब तक हम पूंजीवाद, फासीवाद और समाजवाद — इन तीनों को एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न, अलग-अलग स्वायत्त समाज-व्यवस्थाओं के रूप में नहीं देखेंगे, हम कभी भी फासीवाद के खिलाफ संघर्ष की सही दिशा में सोच-विचार नहीं कर पायेंगे ।
मार्क्स ने कहा था कि उत्पादन का स्वरूप ही किसी भी समाज में आदमी के जीवन का स्वरूप होता है । इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया था कि उत्पादन के साधनों की मिल्कियत अर्थात उत्पादन-संबंध किसी भी समाज के सामाजिक संबंधों, सामाजिक-व्यवस्था को व्यक्त करते हैं । जब हम उत्पादन के स्वरूप के आधार पर ही समाज व्यवस्थाओं पर राय देने लगते हैं तब हम वही भूल करने के लिये मजबूर हो जायेंगे जो भूल हर्बर्ट मारक्यूस से लेकर फ्रैंकफर्ट स्कूल कहे जाने वाले दार्शनिकों ने साठ के दशक में पूंजीवाद और समाजवाद, दोनों को एक ही आधुनिक तकनीक के औद्योगिक युग की समाज-व्यवस्था मान कर, दोनों को समान बता देने की भूल की थी । उन्होंने उत्पादन के साधनों के सामाजीकरण के उस सच की अवहेलना की थी जो समाजवाद को पूंजीवाद से मूलभूत रूप में अलग करता है ।
यही बात फासीवाद के बारे में भी समान रूप से लागू होती है । थोड़ी सी गहराई में जाने से ही हम देख पायेंगे कि फासीवाद उत्पादन संबंधों के उस रूप पर टिका हुआ है जिसमें उत्पादन के साधनों की निजी मिल्कियत के बावजूद उनका तानाशाही शासन की कमांड व्यवस्था से संचालन किया जाता है । हिटलर ने ट्रेडयूनियन आंदोलन को कुचल कर पूंजीपतियों को मजदूरों की सौदेबाजी के दबाव से मुक्त कर दिया, लेकिन इसके साथ ही खुद पूंजीपतियों के लिये भी यह तय कर दिया कि जर्मनी के कारखानों में किस चीज का कितना उत्पादन किया जायेगा; किस प्रकार वे विश्व विजय की हिटलर की योजना की सेवा में लगे रहेंगे । अर्थात, उद्योग चलेंगे पूरी तरह से हिटलर के फरमानों के अनुसार । जैसे भारत में मोदी ने पूरी अर्थ-व्यवस्था को अपनी निजी मुट्ठी में कस लेने के लिये नोटबंदी की तरह का सामान्य रूप से निंदित कदम उठाने में जरा सी भी हिचक का परिचय नहीं दिया । अर्थ-व्यवस्था के सामान्य मान्य नियमों को ताक पर रख कर उसे एक तानाशाह की सनक के अधीन कर देने की यही लाक्षणिकता मोदी और आरएसएस के फासीवादी चरित्र का एक सबसे बड़ा सबूत पेश करती है । हिटलर ने अपने काल में उन सभी उद्योगपतियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था जिन्होंने हिटलर के उदय में उसकी सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता की थी । (देखें, अरुण माहेश्वरी : हिटलर और व्यवसायी वर्ग https://chaturdik.blogspot.in/2016/03/blog-post_10.html)
इसकी तुलना में सामान्य पूंजीवादी जनतंत्र मूलतः उत्पादन के साधनों की निजि मिल्कियत पर टिका होने पर भी वह किसी कमांड व्यवस्था के जरिये नहीं, बल्कि मूलतः बाजार के नियमों से संचालित होता है, जिसमें पूंजी के मूलभूत अधिकार को स्वीकृति के साथ ही सामान्य उपभोक्ता समाज की एक सक्रिय भागीदारी भी हुआ करती है । उपभोक्ता के हितों की रक्षा भी राज्य का एक प्रमुख दायित्व होता है । नागरिक के अधिकार, मानव-अधिकार, कानून का शासन की संगति में ही पूंजीपति और उपभोक्ता के अधिकार भी अपनी न्यायोचितता को प्रमाणित करते हैं ।
इस प्रकार, आधुनिक तकनीक के औद्योगिक युग के एक ही क्षितिज में उभर कर आने वाली इन तीन अलग-अलग समाज-व्यवस्थाओं, पूंजीवादी जनतंत्र, फासीवाद और समाजवाद को हम तात्विक रूप में बिल्कुल तीन अलग-अलग जगहों पर रख कर स्वतंत्र रूप में समझ सकते हैं और इन तीनों व्यवस्थाओं के तहत सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक मान-मूल्यों को भी अलग—अलग करके देखा जा सकता है।
यही वह संदर्भ है जिससे पता चलता है कि जहां से पूंजीवादी जनतंत्र का संकट यदि फासीवाद के आगमन का कारण बन सकता है, वहीं से समाजवाद के द्वार भी खोल सकता है । मूल प्रश्न मनुष्य द्वारा पहले से उपार्जित शक्तियों और अधिकारों की रक्षा से जुड़ा होता है । यह समय और स्थान के एक वृत्त से मुक्त होकर बिल्कुल दूसरे वृत्त में प्रवेश की तरह है । नवंबर क्रांति की विद्रोही विरासत तबाह की जा रही उच्छिष्ट मानव-शक्ति को सामाजिक रूपांतरण की एक नई संगठित, सृजनात्मक शक्ति में बदलने का संदेश देती है। हर समाज में बनने वाले द्वंद्वात्मक संयोगों को मानव-मुक्तिकारी समाज व्यवस्थाओं में उतारना ही क्रांतिकारियों का काम है।जीवन के सभी स्तरों पर मार्क्सवाद के प्रयोग की स्थितियों को समझते हुए उन्हें मूर्त करने में ही यह क्रांतिकारी विज्ञान चरितार्थ होता है।
और, जैसे ही हम समाज-व्यवस्थाओँ और उसमें होने वाले परिवर्तनों की इस प्रकार की एक स्पष्ट तात्विक समझ को हासिल करेंगे, हमें भारतीय राजनीति में पिछले लगभग सत्तर साल से शासन की नीतियों को तय कर रही कांग्रेस पार्टी और आज उसके नेता राहुल गांधी और हिटलर के नाजीवादी एकीकृत शासन की समझ पर चलने वाली आरएसएस और नोटबंदी तथा विकृत ढंग से जीएसटी लागू करने वाले तुगलकी नेता नरेन्द्र मोदी के बीच फर्क करने में कोई कठिनाई नहीं होगी । फासीवाद से लड़ाई को लेकर हमारे सामने तब कोई मानसिक गतिरोध नहीं होगा । हमें मोदी के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में ही व्यापकतम एकजुट आंदोलन की रणनीति से अपने को जोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी । हमारे देश में हमें अपने धर्म-निरपेक्ष और कल्याणकारी राज्य के संविधान की रक्षा की लड़ाई के जरिये पूरे समाज के हितार्थ मनुष्यों की अब तक अर्जित शक्तियों और उनके अधिकारों के प्रयोग को सुनिश्चित करना है। शोषण की ताकतें इस नई परिस्थिति का इस्तेमाल राज्य को अधिक से अधिक दमन-मूलक बनाने के लिये करेगी। हमारे जैसे देश में बेरोजगारों की बढ़ती हुई फौज को गुंडों-बदमाशों (गोगुंडों) की फौज में बदलने की कोशिश आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। इससे दंगाइयों की, अन्ध-राष्ट्रवाद के नशे में चूर आत्म-घाती युद्धबाजों की फौज बनाई जायेगी। लेकिन उतना ही बड़ा सच यह भी है कि यह हिटलर का, औद्योगिक पूंजीवाद के प्रथम चरण का जमाना नहीं है। यह मनुष्यों के आत्म-विखंडन से लेकर समान स्तर पर विखंडित, अकेले मनुष्यों की नई सामाजिकता का जमाना भी है। मूल बात यह है कि हवाई हो या ठोस, मनुष्यों द्वारा अर्जित नई उत्पादन शक्तियों के अनुरूप मानव समाज के नये स्वरूपों के निरूपण को कोई रोक नहीं सकता है। इसका प्रभाव मनुष्यों के सामाजिक जीवन पर जितना पड़ेगा, उससे कम चिंतन के स्तर पर तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा के स्तर तक नहीं पड़ेगा ।
आज जब हम नोटबंदी की तरह के एक चरम तुगलकी कदम से सामान्य जन-जीवन में मची हुई अफरा-तफरी की परिस्थितियों में नोटबंदी की घोषणा के काले दिन के एक साल पूरा होने के दिन की ओर बढ़ रहे हैं, हमें लगता है कि यह जरूरी है कि आधुनिक काल में समाज-व्यवस्थाओं के भिन्न-भिन्न रूपों की विविधताओं की तात्विकता के बारे में हमारी एक समझ बनें ताकि एक बुद्धिजीवी के नाते हम जिस विचारधारात्मक बिंदु पर अपने सामने उलझन की एक अवस्था देखते हैं, उस फांस से हम अपने को मुक्त कर सके, और बिना किसी संशय के अपने वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक दायित्वों का निर्वाह कर सके ।
नोटबंदी के बारे में हमारी यह किताब इस लिहाज से यदि जरा सी भी मददगार साबित हो सके तो हम उसे इसकी सफलता मानेंगे । नोटबंदी के उस दौर के जो चित्र आपको इस किताब में मिलेंगे, उनके ही आत्मिक प्रभावों को आप सरला की इस दौर की कविताओँ में देख पायेंगे, जिसका शीर्षक ही इसकी सारी कहानी को कह देता है — ये जिंदगी की मुर्दा कतारें ।
धन्यवाद ।

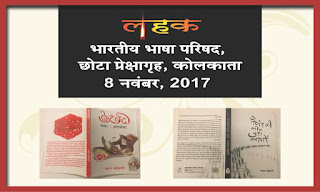

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें