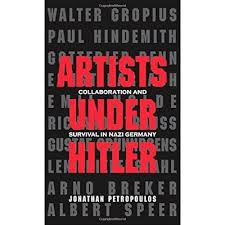- अरुण माहेश्वरी
19वीं सदी के बंगाल के किसी महापुरुष की जिंदगी में झांके और उसके कुल–गोत्र का जिक्र न हो, यह कैसे संभव है? इसकी वजह यह नहीं कि किसी भी हिंदू धर्मावलंबी महापुरुष का जीवन चरित उसके कुलगोत्र की गहराइयों में जाए बिना नहीं समझा जा सकता है। यहां हमारा जोर 19वीं सदी, अर्थात भारत में अंग्रेजी राज के स्थिर होने की सदी, पर है ।
वर्ण व्यवस्था तो हिंदुओं में हजारों सालों से चली आ रही है। जाति विभाजन की निरंतर प्रक्रिया से उसके अंदर की गतिशीलता को भी इधर के इतिहासकारों ने पहचाना हैं। लेकिन दिलचस्प है इस प्राचीन व्यवस्था में अंग्रेजी शासन के योग का फल। प्राचीन पश्चिमी समाज में भले ही वर्ण व्यवस्था की तरह की कोई चिरंतर व्यवस्था न रही हो, लेकिन 19वीं सदी के आधुनिक काल में पश्चिम का शासक वर्ग एक खास प्रकार के जातिवाद (नस्लवाद) के सिद्धांत पर प्रयोग कर रहा था। विभिन्न समुदाय के लोगों की चमड़ी और आंख की पुतली के रंग, उनके ललाट और मस्तक के माप आदि के कथित वैज्ञानिक तौर तरीकों से इस सिद्धांत का ईजाद किया था और उसी के जरिये समाज तथा शासन के क्रम–विन्यास में विधि ने किसके लिये कौन सी जगह तय की है, इसे अनंत काल के लिये स्थिर कर देने का उन्होंने बीड़ा उठाया था। वे नस्ल (जाति)( Race) को इतिहास की कुंजी मानते थे।
कहना न होगा कि इस देश में ब्रिटिश शासन के पैर जमाने के साथ ही अंग्रेजों की इसी ‘वैज्ञानिक’ खुराफात के प्रयोग ने इस समाज पर कम रंग नहीं दिखाया। भारत में 1901 की जनगणना का आयुक्त राबर्ट रिस्ले कहता है, जाति भावना ... इस सचाई पर आधारित है कि उसे वैज्ञानिक विधि से परखा जा सकता है; कि उससे किसी भी जाति को संचालित करने वाले सिद्धांत की आपूर्ति होती है; कि यह शासन के सर्वाधिक आधुनिक विकास को आकार देने के लिये गल्प अथवा परंपरा के रूप में कायम रहती है; और अंत में उसका प्रभाव उसके द्वारा समर्थित खास स्थिति को तुलनात्मक शुद्धता के साथ संरक्षित रखता है।
(...race sentiment...rests upon a foundation of facts that can be verified by scientific methods; that it supplied the motive principle of caste; that it continues, in the form of fiction or tradition, to shape the most modern developments of the system; and, finally, that its influence has tended to preserve in comparative purity the types which it favours. )
जाहिर है कि अंग्रेजों ने भारत की वर्ण व्यवस्था को यहां नस्ली शुद्धता को चिरंतर बनाये रखने के पहले से बने–बनाये एक मुकम्मल ढांचे के रूप में देखा और यहां अपनी शासन व्यवस्था के विकास लिये इसका भरपूर प्रयोग करने का निर्णय लिया। उनकी इसी दृष्टि ने भारत में 1871 का जरायमपेशा जातियों का कानून बना कर कुछ तबको को हमेशा के लिये दागी घोषित कर दिया। और यही वह नजरिया था जिसके चलते 1891 की पहली मदुर्म शुमारी में सिर्फ जातियों की गणना नहीं बल्कि उनकी परिभाषा और व्याख्या को भी शामिल किया गया। कहना न होगा कि जातियों की इन उद्देश्यपूर्ण पहचान की कोशिशों ने भारतीय समाज में ऐसा गुल खिलाया कि यहां के विभिन्न समुदायों में जनगणना के खातों में अपनी जाति को अपने खास ढंग से परिभाषित–व्याख्यायित कराने की होड़ सी लग गयी। समझदारों को यह जानते देर नहीं लगी कि इसीसे यह तय होना है कि आने वाले दिनों में अंग्रेजी शासन की पूरी व्यवस्था में कौन सा समुदाय किस पायदान पर खड़ा होगा; शासन की रेवडि़यों के बंटवारे में किसके कितना हाथ लगेगा। और इसप्रकार, भारतीय वर्ण–व्यवस्था इस नये पश्चिमी नस्लवादी सिद्धांत से जुड़ कर एक अलग प्रकार की जाति चेतना के उद्भव का कारण बनी।
आज हम जिस जातिवाद से अपने को जकड़ा हुआ पाते हैं, उसके बहुत कुछ को भारत में अंग्रेजी शासन की देन कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 19वीं सदी के पहले के इतिहास में जो ब्राण विरले ही कहीं बलशाली, वैभवशाली दिखाई देते हैं; सदा राज–कृपा के मुखापेक्षी और उसीके बल पर यदा–कदा भौतिक दुनिया में भी किंचित महत्व पाते रहे हैं, वे अंग्रेजों की ‘जाति–गणना’ में दखल देकर आदमी के आत्मिक जगत के पूर्ण अधिकारी बन गये। और, इसप्रकार नई शासन व्यवस्था से उनका अपना एक खास रिश्ता बना, वे भी अंग्रेजों के ‘कानून के शासन’ के एक प्रमुख स्तंभ बन गये। अंग्रेजों के संपर्क से बने बंगाल के नवजागरण के तमाम मनीषियों के जीवन में गहराई से उतरिये, ऐसी बहुतसी बातें साफ दिखाई देने लगेगी।
लुब्बेलुबाब यह कि 19वीं सदी के ब्रिटिश राज में हिंदू समाज की जाति– अस्मिता का बोध एक नयी ऊंचाई पर था। ऐसे काल में किसी के गोत्र–कुल की क्या कीमत रही होगी, सहज ही समझा जा सकता है।
इसके अलावा रवीन्द्रनाथ के पूर्वजों का इतिहास जानने की एक और दूसरी महत्वपूर्ण वजह है। इस अध्ययन के जरिये रवीन्द्रनाथ के संपूर्ण व्यक्तित्व की पड़ताल के आधार पर उन पर कोई निश्चित राय बनाने के पहले ही एक बात आसानी से कही जा सकती है कि रवीन्द्रनाथ कहीं से ऐसे इंसान नहीं थे जिनमें एक गुलाम देश के नागरिक की किसी भी प्रकार की कुंठा का लेश मात्र मौजूद हो। स्वतंत्रता उनकी कामना नहीं, उनकी नैसर्गिकता थी। तुलसीदास लिखते है: ‘मति अकुंठ हरि भगति अखंडी’। एक अकुंठ, अखंड और संपूर्ण मानवता को समर्पित रवीन्द्रनाथ के समान विराट वैभवशाली व्यक्तित्व का भारत की तरह के गरीब और गुलाम देश में कैसे निर्माण हुआ, यह किसी के लिये भी विस्मय का विषय हो सकता है।
रवीन्द्रनाथ के इसी व्यक्तित्व के संधान के क्रम में आइये सबसे पहले हम क्यों न रवींद्रनाथ के गोत्र–कुल और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर नजर डाले। संभव है इससे उस विशाल, वैभवशाली जीवन की तहों में प्रवेश के भी कुछ जरूरी सूत्र मिल जाए।
रवीन्द्रनाथ के कुल–गोत्र की तलाश में हम उन आख्यानों अथवा किंवदंतियों के विस्तार में नहीं जायेंगे जो बंग क्षेत्र में ब्राह्मणों के आगमन के बारे में कही जाती है।
इस पूरे संदर्भ में यहां रवीन्द्रनाथ के जीवनीकार प्रभात कुमार मुखोपाध्याय द्वारा प्रणीत चार खंडों में प्रकाशित रवीन्द्र जीवनी के संबंधित अंश में कही गयी बातों का उल्लेख करना ही काफी होगा। उनके अनुसार 11वीं सदी में किसी समय आदिशूर के राज्य में कान्यकुब्ज से शांडिल्य गोत्र के क्षितिश, वत्स्य गोत्र के सुधानिधि, सवर्ण गोत्र के सौभरि, भारद्वाज गोत्र के मेधातिथि और कश्यप गोत्र के बीतराग नामक पंचब्राह्मण महायान बौद्धधर्म के विचित्र विचारों में डूबे बंगदेश में ब्राह्मण धर्म को स्थापित करने के लिये आये थे। ये बंगदेश सिर्फ आये भर थे, लेकिन यहां किसी प्रकार के यज्ञ अथवा दूसरे काम–काज नहीं किये थे। कहते हैं कि इन्हीं के पंचपुत्र भनारायण वेदाध्ययी के बेटे श्री हर्ष और दक्ष से बंगदेश में ब्राण कुल का उद्भव हुआ।
दक्ष की चौदह संतानों में से एक, धीर को आदिशूर के बेटे भूशूर से बंगाल में निवास के लिये गुड़ नामक एक गांव मिला था। आज यह गांव पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद जिले में है। गुड़ गांव के निवासी होने के नाते वे ‘धीरगुड़ी’ अथवा ‘धीरगुड़’ के नाम से जाने जाने लगे। इन्हीं की सातवीं पीढ़ी के रघुपति आचार्य ने वयस्क होने के उपरांत संन्यास ले लिया और ‘दंडी’ बन गये; कहते हैं कि उन्हें काशीवास के काल में दंडी समाज ने कनकदंड भेंट किया था। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि ‘कनकदांड़’ गांव में जाकर बस जाने के कारण परवर्ती दिनों में रघुपति के वंशजों को ‘कनकदंडी गुड़’ कहा जाने लगा। इसी ‘कनकदंडी गुड़’ की एक शाखा का यवनों (मुसलमानों) से संपर्क होने के कारण उन्हें पीराली दोष से दूषित माना गया और इसप्रकार वे ब्राह्मण समाज में पतित समझे जाने लगे।
रघुपति आचार्य की चौथी पीढ़ी के जयकृष्ण ब्रचारी को ही शायद राय की उपाधि मिली थी। जयकृष्ण के दो बेटे थे – नागर और दक्षिणानाथ। दक्षिणानाथ के चार बेटे थे – कामदेव, जयदेव, रतिदेव और शुकदेव। इन्हीं कामदेव भाइयों का मुसलमानों से संपर्क हुआ और वे पीराली होगये। इस समय तक बंगाल में तुर्कों का शासन होगया था और दक्षिणानाथ को राजदरबार से ‘रायचौधुरी’ की उपाधि मिली थी। कामदेव बंधु आज के बांग्ला देश के जसहोर जिले के चेंगुटिया परगना के जमींदार थे। जाहिर है कि नाना कारणों से हिंदुओं के विभिन्न समुदाय विजेता शासकों के संपर्क में आये। और यवनों के साथ इस प्रकार से संपर्क में आये अनेक परिवारों को तब हिंदू समाज से अलग कर दिया गया था। सेरखानी, पिराली, श्रीमंथानी, आदि समुदायों का उद्भव इसी प्रकार हुआ।
सवाल उठता है कि आखिर यह पीराली क्या बला है? अगर हम इसकी तह में जाए तो भारतीय समाज में जातियों के उद्भव और विकास के अपने एक बेहद रोचक और उतने ही यातनापूर्ण आख्यान के सूत्रों को भी पकड़ पायेंगे। किसका किससे मेल होने अथवा कौन सा पेशा अपना लेने पर जातिगत पैमाने पर कौन क्या होता रहा है, इसकी सचमुच अपने आप में एक अनोखी दास्तान है। लेकिन जातियों के विभाजन की यह निरंतर प्रक्रिया ही वर्ण व्यवस्था के अंदर की किंचित गतिशीलता का भी एक प्रमुख कारण रही है। ‘पीराली’ भी, कहते हैं, ऐसे ही एक खास प्रकार के मेल–जोल और वहिष्कार–निष्काशन का परिणाम था। इसमें बहुत कुछ समाज के पंडे बने ब्राह्मणों की मनमर्जी का परिणाम भी रहा है। खास तौर पर यवनों के संपर्क में आने के कारण कुछ परिवारों को समाज के इन पंडों ने सम्मान का स्थान दिया, तो इसी कारण से कुछ को पूरी तरह से समाज से वहिष्कृत करके पतित करार दिया। ‘पीराली’ भी ऐसे ही पतित ब्राह्मणों में एक थे। पीराली ब्राह्मण की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि तुर्कों के शासन के दिनों में खान जहां अली नामका एक व्यक्ति दक्षिण बंगाल के सुंदरीवन (आज के बांग्लादेश के खुलना के सुंदरवन) में उपनिवेश कायम करने की सनद लेकर आया था और इसी सनद पर उसे चेंगुटिया परगना की जमींदारी मिली। इन खान जहां के पास ताहेर नामका एक व्यक्ति आया जो पहले ब्राण था, लेकिन एक मुसलमान महिला के प्रेम में पड़के इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। वह नवद्वीप के निकट के पिरलिया अथवा पिरल्या गांव का निवासी था। पिरल्या गांव का निवासी होने के नाते लोग उसे पिरल्या खां कह कर पुकारने लगे। ताहेर कार्यपटु और दक्ष व्यक्ति था, इसीलिये खान जहां ने उसे दीवान बना कर जसहोर बुला लिया था। इसी ताहेर के यहां उपरोक्त दक्षिणानाथ के दो बेटे कामदेव और जयदेव प्रमुख कर्मचारी के पद पर नियुक्त हुए।
कहते हैं कि एक दिन रोजा के समय ताहेर उर्फ पीरअली एक नींबू की सुगंध ले रहा था। उसी समय कामदेव ने मजाक में कहा कि शास्त्रों के अनुसार गंध लेना आधे भोजन के समान है। इसीलिये आपका रोजा टूट गया है। ताहेर मुसलमान होने पर भी ब्राह्मण की संतान था। वह कामदेव के मजाक को फौरन समझ गया, लेकिन उसने विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बाद एक दिन उसने एक मजलिस बुलाई जिसमें ब्राह्मणों सहित तमाम जाति के लोगों को आमंत्रित किया था। इस जलसे में चारों ओर से मुगलाई खाने की गंध फैली हुई थी, जिसे हिंदू सहन नहीं कर पारहे थे। कई लोग कपड़े से नाक को ढक कर बाहर निकल गये। लेकिन चालाक पीरअली ने कामदेव और जयदेव को पकड़ लिया और कहा कि सुगंध से यदि आधा भोजन हो जाता है तो निश्चित तौर पर गोमांस की गंध लेकर तुमने अपनी जाति गंवा दी है। इन दोनों भाइयों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पीरअली के लोगों ने उन्हें दबोच कर उनके मूंह में उस प्रतिबंधित मांस को ठूस दिया और इसप्रकार, वे दोनों ही जाति–च्युत होगये। इसके बाद से ही कामदेव को कमाल खान और जयदेव को जमाल खान के नाम से जाना जाने लगा। पीरअली ने दोनों को जागीर भी दिलवा दी। पीरअली की उस महफिल में और भी जो लोग उपस्थित थे, उनके दुश्मनों ने उन्हें ‘पीराली’ घोषित करके समाज से निकाल दिया। उनमें से भी जिनके पास रुपयों की ताकत थी, वे तो समाज के पंडों की कृपा से फिर से जाति में वापस आगये, और जो किसी भी वजह से इन पंडों को खुश नहीं कर पायें वे ‘पीराली’ बन कर समाज से वहिष्कृत रहे।
कामदेव, जयदेव के दो अन्य भाई रतिदेव और शुकदेव रायचौधुरी अपने दक्षिणडीही के घर में रहते थे। रतिदेव ने समाज के अत्याचारों से दुखी होकर गांव छोड़ दिया। शुकदेव को भी भारी कष्ट उठाने पड़े। नाना छल–चतुराई से शुकदेव ने अपनी बेटी और भतीजी का ब्याह किया। बेटी का विवाह एक श्रेष्ठ श्रोत्रिय जाति के नौजवान, पीठाभोग के जमींदार जगन्नाथ कुशारी से किया और भतीजी का विवाह फुलिया के एक मुखुटी से कर दिया। एक पतित ब्राह्मण परिवार में विवाह करने के कारण जगन्नाथ को उसके कुटुंब और जाति से वहिष्कृत कर दिया गया और वह पीठाभोग के बजाय दक्षिणडीही में अपने ससुराल में रहने लगा। शुकदेव ने अपने जंवाई को पूरी इज्जत बख्शी और आज के बारोपाड़ा नरेन्द्रपुर गांव के उार में उारपाड़ा नामका एक गांव उसे दान में दे दिया। इसप्रकार शुकदेव की भतीजी और बेटी के विवाह से ब्राणों की ‘पीराली’ शाखा चल पड़ी।
कहा जा सकता है कि बंगाल के ठाकुर परिवार के आदिपुरुष ये जगन्नाथ कुशारी महाशय ही थे जो अपने ब्याह के चलते पीराली समाज में शामिल होगये थे। जगन्नाथ के दूसरे बेटे पुरुषोत्तम से ठाकुर वंश की परंपरा चली। पुरुषोत्तम के पोते रामानंद के दो बेटे महेश्वर और शुकदेव के समय से यह ठाकुर परिवार कोलिकाता निवासी होगया।
इस बारे में कहानी यह है कि जाति के कारण झेल रहे अपमान की वजह से ही महेश्वर और शुकदेव अपने गांव बारोपाड़ा से निकल कर कोलिकाता गांव के दक्षिण में गोविंदपुर में आकर बस गये। तब तक अंग्रेजों को गोविंदपुर, सुतानाटी और कोलिकाता नामक तीन गांवों की सनद मिल चुकी थी। अंग्रेजों के वाणिज्यिक जहाज इसी गोविंदपुर की गंगा में ही आकर लगा करते थे। उन दिनों कोलिकाता और सूतानाटी में सेठ बसाक नामके एक प्रसिद्ध व्यापारी हुआ करते थे। अंग्रेज कप्तानों के इन जहाजों से माल–असबाब की ढुलाई–लदाई और खाने–पीने की व्यवस्था का काम पंचानन कुशारी किया करते थे। इन सभी मेहनत के कामों में स्थानीय हिंदू समाज की तथाकथित निम्न जातियों के लोग उनके लिये काम करते थे। ये लोग एक ब्राह्मण भले आदमी को उसके नाम से पुकारने में हिचकते थे, इसीलिये वे पंचानन को ‘ठाकुर मोशाय’ कह कर पुकारने लगे। इसीसे जहाज के कप्तान उसे पंचानन ठाकुर के नाम से जानने लगे। अपने कागजातों में उन्होंने उसके नाम के साथ Tagore, Tagoure लिखना शुरू कर दिया और इसप्रकार ‘कुशारी’ पदवी का स्थान ‘ठाकुर’ पदवी ने ले लिया।
पंचानन ठाकुर के दो बेटे हुए – जयराम और रामसंतोष तथा शुकदेव के एक बेटा, कृष्णचंद्र। अंग्रेज व्यापारियों से तीनों ने थोड़ी अंग्रेजी सीखी। इसके अलावा उन दिनों फ्रेंच भाषा का भी अच्छा–खासा चलन था। 1742 में कोलिकाता की पैमाईश का काम शुरू हुआ और जयराम तथा रामसंतोष अमीन के पद पर नियुक्त होगये। इसी कारण से खुलना में इनका पैतृक निवास ‘अमीन का निवास’ के नाम से प्रसिद्ध है। उसी समय कंपनी ने ‘फोर्ट विलियम’ के निर्माण का काम शुरू किया था। सरकार के जिस विभाग को निर्माण का यह काम सौंपा गया था, जयराम उस विभाग से जुड़े हुए थे। ‘फोर्ट विलियम’ की इस इमारत को बनाने में तब बेशुमार पैसा खर्च हुआ था और इसके पूरा होने में भी अनुमान से काफी ज्यादा समय लगा था। कहते है कि उन दिनों कंपनी के अधिकारियों से लेकर साधारण गुमाश्ते तक में ईमानदारी नामकी कोई चीज नहीं हुआ करती थी और ‘फोर्ट विलियम’ की इमारत को बनाने में चीफ इंजीनियर से लेकर सरदार मिस़्त्री तक सबने काफी धन कमाया था। जयराम ने इस काम में क्या कमाया इसके बारे में कोई पक्की जानकारी न होने पर भी यह सच है कि उन्होंने उसी काल में धनसाय (आज के धर्मतल्ला, शहीद मीनार) में मकान बनाया, जमीनें खरीदी और फोर्ट विलियम्स के पास ही गंगा के तट पर एक बगान बाड़ी बनायी। वे जब मरे तब धन–संपिा के लिहाज से काफी अच्छे थे। जयराम ठाकुर के तीन बेटे थे – नीलमणि, दर्पनारायण और गोविंदराम। उन्होंने अपने बड़े बेटे आनंदीराम को त्याग दिया था, जिसके दो बेटे थे।
कोलिकाता पर जब सिराजुद्दौल्ला ने हमला किया तब जयराम ने अपनी चल संपकिंतु, सोने के गहनों आदि को फोर्ट विलियम्स में जमा करा दिया था। उस हमले में धनसाय के घर को भी कोई नुकसान नहीं पंहुचा था। 1756 में जयराम की मृत्यु के थोड़े दिनों बाद ही नीलमणि आदि ने अपने पूर्वजों की धनसाय की संपत्ति को 5 हजार रुपयों में बेच दिया। 1757 में पलाशी की लड़ाई के बाद मीरजाफर अलि खां बंगाल सूबे के नवाब बने और सिराजुद्दौल्ला के हमले से हुई शहर की तबाही के मुआवजे के तौर पर उन्होंने ब्रिटिश कम्पनी को भारी रकम अदा की। उसी कोष में से ड्रेक साहब ने जयराम अमीन के बेटों को छ: हजार रुपये दिलवा दिये। जयराम के बेटों के पास इससे कुल 13 हजार रुपये की नगद संपत्ति होगयी। 1764 में इन्हीं बेटों ने कोलिकाता गांव के पाथुरियाघाटा क्षेत्र में जमीन खरीद कर अपना घर बनाया और 13 हजार रुपयों से कंपनी के कागजात खरीद कर अपने गृहदेवता श्रीश्री राधाकांत जीओ के नाम से एक धर्मादा खाता तैयार कर दिया। इन रुपयों पर मिलने वाले ब्याज से देवपूजा के खर्च की व्यवस्था होती थी।
नीलमणि और दर्पनारायण अपने पाथुरियाघाट के आवास के दिनों में साहबों के दीवान बन गये। बड़े भाई दर्पनारायण तो घर पर रह कर पुरखों की संपत्ति को सम्हाले हुए थे। छोटा भाई नीलमणि कमाई के लिये कलकत्ते के बाहर निकल गया। उसने पहले एक जिला अदालत में अधीनस्थ अमले के रूप में काम किया और धीरे–धीरे सेरिस्तदार के पद तक चला गया। उन दिनों कोई भी देशी आदमी सरकार में इससे बड़े पद की उम्मीद नहीं कर सकता था। इसके अलावा, तब धन होने मात्र से समाज में मान नहीं मिलता था। कोलिकाता में पैसेवालों को ‘बाबू’ कहा जाता था। कुलीनों की जमात में जगह तभी मिलती थी जब किसीके पास जमींदारी हो। नीलमणि ने सेरिस्तदार के पद पर रहते हुए जो कमाई की उसीसे ठाकुर परिवार में वस्तुत: जमींदारी का श्रीगणेश किया। उनकी अगली पीढ़ी के राममणि ने भी उड़ीसा में थोड़ी जमींदारी खरीदी; फिर उनके भाई राम वल्लभ ने उसमें और संपत्ति जोड़ी। लेकिन जिसे वास्तव में जमींदार का ओहदा कहते है, वह सम्मान नीलमणि के पोते, द्वारकानाथ को ही मिला।
बहरहाल, पाथुरियाघाट का संयुक्त परिवार एकदिन टूट गया। इसके मूल में संपत्ति का मसला था। नीलमणि बाहर से हर महीने अपने बड़े भाई को अपनी बचत से रुपये भेजा करता था। लेकिन जब वह सरकारी सेवा से निवृत्त्त हुआ, तब इन्हीं रुपयों के हिसाब को लेकर दोनों भाइयों के बीच मनमुटाव होगया। बाद में समझौता हुआ तो नीलमणि एक लाख रुपया नगद लेकर पाथुरियाघाट का मकान और धर्मादे की संपति छोड़ अपने छोटे भाई से अलग होगये। नीलमणि ने जोड़ाबगान के कर ब्राण वैष्णवचरण सेठ से जोड़ासांकू में घर बनाने के लिये एक बीघा जमीन ली और सन् 1784 के जून महीने से उनका परिवार वहीं जाकर रहने लगा। कहा जाता है कि चूंकि नीलमणि खुद पक्के ब्राण थे, इसीलिये वैष्णव सेठ ने उन्हें बहुत मामूली कीमत पर जोड़ासांकू की जमीन दे दी थी। वैष्णव सेठ किस प्रकार के ब्राण थे, यह अकेले इस तथ्य से जाना जा सकता है कि वे कलको में शुद्ध गंगा जल के संरक्षक माने जाते थे और उसके सबसे बड़े निर्यातकर्ता थे। कलको से बाहर जहां गंगा जल नहीं मिलता था, वहां गंगा जल से भरे उन्हीं घड़ों को शुद्ध माना जाता था, जिन पर वैष्णव सेठ की मोहर लगी होती थी। बहरहाल, रवीन्द्रनाथ ठाकुर को जिस जोड़ासांकू के ठाकुर परिवार से जोड़कर हम देखते हैं, उस परिवार की परंपरा इसी जोड़ासांकू के मकान से शुरू हुई थी। अर्थात, जयराम ठाकुर के दूसरे बेटे नीलमणि ठाकुर को जोड़ासांकू के ठाकुर परिवार का आदिपुरुष, उत्स कहा जा सकता है।
नीलमणि के तीन बेटे और एक बेटी थी : रामलोचन, राममणि, रामवल्लभ, और कमलमणि। नीलमणि की अपनी सामाजिक और आर्थिक प्रतिष्ठा के चलते उन्होंने अपनी बेटी का विवाह तो एक आस्थावान हिंदू परिवार में कर दिया लेकिन बेटों की शादी पीराली समाज में ही करनी पड़ी।
नीलमणि के बाद ठाकुर परिवार के मुखिया बने रामलोचन। उनकी अपनी कोई संतान न होने के कारण उन्होंने अपने भाई राममणि के बेटे द्वारकानाथ को गोद ले लिया। राममणि ने दो शादियां की थी। पहली पत्नी मेनका देवी से राधानाथ, जावी देवी, रासविलासी और द्वारकानाथ पैदा हुए तथा दूसरी पत्नी दुर्गामणि से रमानाथ और सरस्वती देवी का जन्म हुआ। रामलोचन अपने जमाने के एक संभ्रांत भद्रजन थे। प्रभातकुमार मुखोपाध्याय के शब्दों में अपनी वेशभूषा के ढंग, सांध्य–भ्रमण, संगीत प्रेम आदि तत्कालीन कुलीनों के लक्षण उनमें दिखाई देते थे।
जाहिर है कि इस पूरे लेख में हमने रवीन्द्रनाथ ठाकुर के कुल-गोत्र, वंश परंपरा और उनके परिवार की सामाजिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा की हैं। फिर भी हमारा मक़सद सिर्फ़ उनके वंश का इतिहास बताना नहीं है। हम इसे एक ऐसी ज़मीन की तरह देखना चाहते हैं, जहाँ से उनके व्यक्तित्व और उनके स्वतंत्र स्वभाव की जड़ें पोषित होती हैं।
रवीन्द्रनाथ जिस ठाकुर परिवार से आते हैं, उस परिवार की नींव में ही एक विचित्र का द्वंद्व-बीज पड़ गया था – उसे कभी समाज के ऊपरी कुलीन तबकों में गिना जाता था, तो कभी जाति से बाहर कर ‘पीराली’ कह कर अपवर्जित कर दिया गया । इसी खींच-तान ने उस परिवार की सामाजिक आकांक्षा, असुरक्षा और नवाचार की एक खास गति तय की। यही पृष्ठभूमि आगे चलकर रवीन्द्रनाथ के आत्मविश्वास, खुलेपन और स्वतंत्र चेतना की नींव बनती है।
फ्रांसीसी विचारक और मनोविश्लेषक जॉक लकान का एक सिद्धांत है—नाम-का-पिता।(name-of-father, le Nom-du-Père) इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ़ अपने जैविक पिता से नहीं, बल्कि उस सामाजिक नाम, उस मान्यता और उस प्रतीकात्मक स्थिति से बनता है जो पिता के माध्यम से उसे समाज में मिलती है। यह नाम—यानी ‘पिता का नाम’—व्यक्ति को भाषा, परंपरा और कानून के संसार से जोड़ता है और उसकी इच्छा, उसके आत्मबोध को एक दिशा देती है।
ठाकुर परिवार में यह ‘पिता का नाम’ कई बार टूटा, बदला और फिर से बना। यही प्रक्रिया, जो कभी अपमान में और कभी प्रतिष्ठा में घटित हुई, बाद में रवीन्द्रनाथ के मनोविकास में एक गहरे आत्मबोध का कारण बनी। रवीन्द्रनाथ सामाजिक प्रतिष्ठा के सर्वोच्च शिखर पर जाकर भी ‘पिरालीपन’ की पीढ़ियों पुरानी स्मृति को त्याग नहीं पाते हैं । इसने उनमें एक ऐसे सनातन विद्रोही भाव को बनाये रखा जिससे वे न कभी गुलाम नागरिक की मानसिकता से दबे, न किसी जातिगत कुंठा से। वे अपने नाम को, अपनी जगह को, अपने काव्य और चिंतन से खुद गढ़ते चलते गए।
इस लेख को इसी नज़र से पढ़ा जाना चाहिए कि ठाकुर परिवार की यह पूरी ऐतिहासिक यात्रा, अपने आप में रवीन्द्रनाथ के आत्म-निर्माण के प्रस्थान की एक प्रतीकात्मक कथा है—जहाँ सामाजिक यथार्थ और मनोविश्लेषण मिलकर एक ऐसे व्यक्तित्व की रचना करते हैं जो स्वभावतः स्वतंत्र है, और जिसकी चेतना आधुनिक भारत के लिए एक नया नाम बन जाती है।
ठाकुर परिवार का इतिहास, जैसा कि हमने देखा, न सिर्फ़ कुलीनता-अकुलीनता के पारंपरिक द्वंद्व में उलझा हुआ था, बल्कि एक ऐसे ऐतिहासिक क्षोभ से भी संचालित था जिसमें जाति, वंश और सत्ता के सभी प्रतीक एक प्रकार की अस्थिरता और अपवर्जन (exclusion) से गुजरते रहे। इसी द्वंद्व में, लकान के ‘नाम-का-पिता’ की अवधारणा एक विशेष महत्व ग्रहण करती है। यह कोई जैविक या नैतिक सत्ता नहीं, बल्कि वह सांस्कृतिक, प्रतीकात्मक (symbolic) कार्य है जो प्रमाता को संरचित करता है, उसे सामाजिक भाषा, उत्तराधिकार और कानून की दुनिया में स्थान प्रदान करता है। ठाकुर वंश में यह प्रतीकात्मक पिता-स्थान एक बार नहीं, कई बार विचलित होता है—पीराली ब्राह्मणों के रूप में बहिष्कृत, फिर अंग्रेज़ी प्रशासन में उच्च पदों द्वारा पुनः प्रतिष्ठित।
इस ‘अव्यवस्थित पितृत्व’ (dislocated paternity) के बावजूद, जब द्वारकानाथ ठाकुर अकूत धन-संपत्ति इकट्ठा करके प्रिंस कहलाने लगते हैं और देवेन्द्रनाथ एक आधुनिक धार्मिक विचार (ब्रह्मो समाज) के प्रतिनिधि बन जाते हैं, तब यह पिता का नाम पुनः प्रतिष्ठित होता है— इसकी "प्रतीकात्मक व्यवस्था" की पुनर्स्थापना । यही क्रम रवीन्द्रनाथ में आकर एक ऐसे सृजनात्मक अधिनियम का रूप ले लेता है, जिसमें पिता का नाम केवल उत्तराधिकार नहीं बल्कि आत्म-पहचान, स्वयं से अर्जित नाम में रूपांतरित हो जाता है।
रवीन्द्रनाथ के जीवन में ‘नाम-का-पिता’ की लकानियन क्रिया एक ऐसी स्थिति तैयार करती है जिसमें वे न तो जातिगत कुंठा के शिकार होते हैं और न ही सत्ता की आकांक्षा से बंधते हैं। वे एक "मुक्त प्रमाता" (free subject) की तरह उस ‘प्रतीकात्मक अभाव’ को आत्मसात करते हैं जिसकी गति उन्हें न सिर्फ़ आधुनिक भारत के सांस्कृतिक प्रमाता के रूप में स्थापित करती है, बल्कि उन्हें एक ‘समाज-सृष्टा कवि’ (poet as lawgiver) बना देता है। इसप्रकार, ठाकुर वंश के भीतर घटित यह प्रतीकात्मक प्रक्रिया, कुलीनता और अकुलीनता के बीच के सभी संक्रमणों को पार करती हुई, रवीन्द्रनाथ के आत्म-निर्माण का वह धरातल प्रदान करती है जिसे हम लकान के शब्दों में एक नाम का मिलना कह सकते हैं—एक ऐसा नाम जो ‘अकुंठ मानव’ के खुले आसमान की तरह उन्मुक्त होता है।
संदर्भ
1. Lacan, Jacques. Écrits एवं The Psychoses: The Seminar of Jacques Lacan Book III. अनुवाद एवं संपादन: Jacques-Alain Miller. Routledge.
2. मुखोपाध्याय, प्रभात कुमार. रवीन्द्र-जीवनी, चार खंडों में. विश्वभारती प्रकाशन.
3. Risley, Herbert Hope. The People of India (1908).
4. चक्रवर्ती, निलमणि. Banglar Brahman O Brahmanitva (बांग्ला में).
5. Tagore, Rabindranath. My Reminiscences (1917).
6. Bhattacharya, Sabyasachi (Ed.). The Mahatma and the Poet: Letters and Debates Between Gandhi and Tagore 1915–1941.