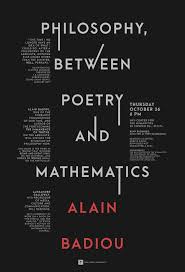—अरुण माहेश्वरी
कोरोना और भारत में लॉक डाउन के अमेरिकी पहलू पर हमारे लेख पर कुछ नजदीकी मित्रों ने हमसे कहा कि आप कब से इस प्रकार की कांसपिरेसी थ्योरी पर विश्वास करने लगे है !
यह सच है कि हम बीजेपी के सुब्रह्मण्यम स्वामी की तरह किसी भी सरकार या राजनीतिक दल के हर नीतिगत निर्णय के पीछे किसी न किसी साजिश का संधान करने के नजरिये के सख्त विरोधी रहे हैं । इस बात को समझते हुए भी कि दुनिया में चल रहे कौन से विमर्श और खास तौर पर प्रभुत्वशाली देशों की सरकारों के क्रियाकलाप हमारे देश की राजनीति की किस धारा को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, हमने हमेशा उन सबकों समग्र रूप से अपने ही राजनीतिक परिवेश के अंग के रूप में देखा हैं, हमें न किसी भी सार्वभौम सरकार के आर्थिक-राजनीतिक फैसलों के पीछे शुद्ध रूप से किसी बाहरी ताकत के निर्देश का पालन नजर आता है और न ही हर दल के राजनीतिक फैसलों के पीछे देश के ही किसी वर्ग विशेष की सीधी हुक्म फरमानी ।
पर इससे कौन इंकार कर सकता है कि जीवन के हर क्षेत्र की तरह ही राजनीति के क्षेत्र में भी विचारधाराओं के नाना रूपों की एक सक्रिय उपस्थिति होती है । उनके अनुसार नई संभावनाओं को साकार करने अनेक प्रकार के प्रयोग किये जाते हैं । वामपंथी हो या दक्षिणपंथी ताकतें, सब काल और स्थान के अपने अनुमानों के अनुसार आगे के रास्तों की तलाश में रहते हैं । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमेशा इसी प्रक्रिया के जरिये एक गतिशीलता बनी रहती है । सफलताओं और विफलताओं के रोज नये किस्से लिखे जाते रहते हैं ।
यही वजह है कि जब सुब्रह्मण्यम स्वामी की तरह के साजिश संधानी भारत की आर्थिक नीतियों के पीछे विश्व बैंक और अमेरिका स्थित अफसरों की भूमिका की अपने ढंग से चर्चा करते हैं, तो हम उससे यह नहीं समझते कि उन अधिकारियों के जरिये अमेरिकी सरकार भारत सरकार को चला रही है, भारत सरकार अमेरिका की गुलाम बन चुकी है, बल्कि उससे हम सिर्फ इतना ही ग्रहण करते हैं कि अमेरिका में शासन-नीतियों के प्रभुत्वशाली हलकों में सामाजिक-आर्थिक विषयों पर अभी जो चर्चाएं चल रही है, वहां से प्रशिक्षित हो कर आए अधिकारियों के जरिये उन चर्चाओं से बनने वाली सारी अवधारणाएँ किसी न किसी रूप में यहां की शासकीय नीतियों पर भी अपनी छाया डाल रही है, और निश्चित तौर पर भारत के अपने काल और स्थान के यथार्थ बोध को प्रभावित कर रही है ।
बस, इसी हद तक हम अमेरिका हो या कोई दूसरा देश हो, हमारे देश के शासन की नीतियों पर उनके प्रभाव को देखते हुए उसे अपने विवेचन का विषय बनाते हैं ।
हम इस बात से कभी इंकार नहीं कर सकते हैं कि दुनिया के पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक विषयों पर तमाम स्तरों पर जो विचार-विमर्श चल रहे हैं, उनसे पूरी तरह आंख चुरा कर तो कोई एक कदम भी नहीं चल सकता है । वह तो एक प्रकार का जीवन से पलायन का सुख लेने वाला शुद्ध ‘बाबावाद’ होगा । इसमें देखने की जरूरत सिर्फ इतनी है कि किस हद तक हम अपने देश के सच को सामने रखते हुए वैश्विक विमर्शों से सामने आने वाली किन्हीं नीतियों को ग्रहण करते हैं या उनसे अस्वीकार करते हैं ।
इस मामले में हम मोदी शासन की सबसे बड़ी कमजोरी यह पाते हैं कि उसने आने के साथ ही सरकार की आंख और कान के रूप में काम करने वाली सारी सांख्यिकी संस्थाओं के कामों में बाधा डालनी शुरू कर दी जिनके चलते शासन के पास भारतीय जीवन के यथार्थ की ही सच्ची और तथ्यमूलक तस्वीर पहुंचनी बंद होने लगी । उसने अपने तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए अर्थनीति के तथ्यों को विकृत करना और सामाजिक सचाई को सामने लाने वाले अध्ययनों को छिपाना शुरू कर दिया । रोजगार और मानव विकास सूचकांक के तथ्यों तक से छेड़छाड़ शुरू कर दी । मोदी जी ने आंकड़ों और तथ्यों का अपना ही एक अलग कल्पित संसार बना लिया, जिसमें भारत की दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थ-व्यवस्था, एक विशाल सैन्य शक्ति, अंतरीक्ष में डग भरने वाली वैज्ञानिक उपलब्धियों वाली चमकती हुई छवि ही प्रमुख हो गई, यहां की गरीब जनता का सच एक सिरे से गायब होता चला गया ।
गरीब लोगों को उनकी जिंदगी में सुधार के बजाय धर्म और सांप्रदायिक उत्तेजना के जरिये वोट के समय अपने पक्ष में करके इसने जनतंत्र के अर्थ को ही बदलना शुरू कर दिया । जनतंत्र एक ऐसा शासन, जिसमें सत्ताधारियों को उस जनता के जीवन में उन्नति के लिये काम करना होता है जो अपने हितों के बारे में पूरी तरह से सचेत नहीं होती है, उसे मोदी ने जनता को सिर्फ उत्तेजित करके एक प्रकार की मूर्च्छना की दशा में डाल कर उस पर अपना प्रभुत्व कायम करने के औजार में बदल डाला । जैसे राजा की अमूर्त उपस्थिति ही उसके प्रति प्रजा में निष्ठा का भाव पैदा किया करता था, मोदी ने उसी फार्मूले का प्रयोग शुरू किया । आधुनिक दुनिया में इसके सबसे बुरे उदाहरण हिटलर और मुसोलिनी के रहे हैं जिन्होंने अपने लोगों को युद्ध में उतार कर करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था । आरएसएस के इतिहास से परिचित लोग जानते हैं कि इसका गठन ही किस प्रकार हिटलर और मुसोलिनी के विचारों की प्रेरणा से किया गया था ।
बहरहाल, ये ही वे प्रमुख कारण रहे हैं, जिनके चलते मोदी ने अपने इन छः सालों के शासन में जो भी फैसले किये, उनमें उन्होंने कभी भी भारत की व्यापक गरीब जनता के हितों को सामने रख कर विचार करने की कोई जरूरत नहीं महसूस की । उनके सामने हमेशा एक अमेरिकी मॉडल रहता है, क्योंकि उससे गहराई से परिचित लोग ही उनके सलाहकारों में अधिक से अधिक हैं । वहां के अकादमिक जगत में विभिन्न आर्थिक विषयों पर जिस प्रकार की चर्चाएँ चलती हैं, वे ही प्रच्छन्न रूप में सरकार की नीतियों में प्रवेश कर जाती है ।
जिस समय मोदी ने नोटबंदी का कदम उठाया उस समय उनके शासन के दो साल बीत चुके थे और हासिल के नाम पर वे नया कुछ भी नहीं दिखा पाए थे । इसकी वजह थी कि वे सत्ता के गलियारों में पहुंचने के पहले तक उस आरएसएस के प्रचारक थे जिसमें भारत की आर्थिक-सामाजिक नीतियां किसी गहरे विमर्श का विषय नहीं बना करती है । वे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को, उसमें भी हिंदू-मुस्लिम संघर्ष को ही भारतीय समाज की धुरि मानते रहे हैं । इसीलिये देश की केंद्रीय सत्ता पर आने के बाद उनके लिये पुराने काल की लीक से हट कर कुछ भी नया करने की कोई दृष्टि ही नहीं थी । उल्टे उनके आने के बाद, बैंकों और निवेश का संकट और भी तेजी से बढ़ने लगा था । ऐसे में, तेजी से बीतते समय की हड़बड़ी में मोदी ने अपने कुछ चार्टर्ड एकाउंटेंट अर्थशास्त्रियों और खुद के सीमित ज्ञान, हिटलर की नाजी अर्थनीति की समझ के साथ अभी पश्चिम की दुनिया में नगदी पर नियंत्रण के बारे में चलने वाले विमर्शों के सूत्र को पकड़ कर नोटबंदी के उद्भट कदम से एक तीर से दो शिकार करने का अभिनव रास्ता अपनाया — बैंकों का पूंजी का संकट दूर होगा और काला धन सामने आने से आगे राजस्व और निवेश में भी कमी नहीं आएगी । न उन्होंने भारत में नगदी के प्रचलन के बारे में तथ्यों को टटोला, न इससे अनौपचारिक क्षेत्र और उसके मजदूरों पर पड़ने वाले प्रभावों पर जरा भी विचार किया । ऐसा लगता है कि अर्थ-व्यवस्था में इन क्षेत्रों के योगदान के विषयों पर उनमें न्यूनतम समझ का भी अभाव था । सत्ता के मद में नोटबंदी की घोषणा करके वे सीधे जापान चले गए और वहां बैंकों के सामने रोते-बिलखते लोगों पर महाबली रावण की मुद्रा में ठठा कर हंसने लगे ।
इसी प्रकार जीएसटी के कदम के पहले भी उन्होंने न अपनी सरकारी मशीनरी का कोई जायजा लिया और न इसके अन्य तात्कालिक और दूरगामी प्रभावों पर विचार किया । मनमोहन सिंह सरकार जीएसटी के बारे में दो साल से विचार ही कर रही थी, लेकिन महाबली ने उसे एक झटके में लागू कर दिया ।
और अब आया है यह कोरोना का संकट । यह एक वैश्विक संकट है और इसके तेजी से संक्रमण के सच को समझते हुए सारी दुनिया के चिकित्सक, जब तक इसका कोई इलाज या टीका नहीं निकल जाता, इससे लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य बता रहे हैं । चिकित्सकों की बात एक वैज्ञानिक सच है । लेकिन फिर भी उतना ही बड़ा सच यह भी है कि राजनीतिशास्त्र चिकित्साशास्त्र नहीं है ।
जिस दिन डब्लूएचओ ने कोरोना महामारी की रोकथाम के बारे में अपनी असहायता को व्यक्त किया था, उसके दूसरे दिन ही 2 मार्च को हमने फेसबुक पर इसके सभ्यता की गति पर पड़ने वाले परिणामों का अनुमान लगाते हुए अपनी एक पोस्ट में लिखा था —
“डब्बूएचओ ने कहा है कि कोरोना वायरस को रोकने की संभावनाएँ कम होती जा रही है । मक्का में विदेशी हज यात्रियों का प्रवेश रोक दिया गया है । वेनिस में कार्निवल का कार्यक्रम स्थगित । ईरान में जुम्मे की नमाज़ के लिये मस्जिदों में इकट्ठा होना रोक दिया गया है । ब्रिटेन में सरकार अपने हाथ में कुछ आपातकालीन अधिकार ले रही है ताकि नागरिकों के आने-जाने को नियंत्रित कर सके । अर्थात् नागरिकों के लिये अभी एक नई संहिता बनने जा रही है । लोग भीड़ और मेलों से बचे ; ग़ैर-ज़रूरी यात्राएँ न करे; एक प्रकार की आत्म-अलगाव की स्थिति को अपनाएँ । जो भी सरकार लोगों में खुद ऐसी चेतना पैदा नहीं करेगी, वह इस महामारी से लड़ने में विफल रहेगी । जनतंत्र के इस काल की सरकारों के सामने यह एक सबसे बड़ी चुनौती होगी । कोरोना वायरस एक नई विश्व आचार-संहिता का सबब बनता दिखाई दे रहा है । यह अब तक के विश्व वाणिज्य संबंधों को भी एक बार के लिये उलट-पुलट देगा । यह शिक्षा, स्वास्थ्य नीतियों पर भी गहरा असर डाल सकता है । स्कूलों-कालेजों और अस्पतालों के स्वरूप पर भी क्रमश: इसका असर पड़ सकता है ।"
राजनीति का लक्ष्य समग्र रूप से जनता के हितों की रक्षा करना है और उसमें चिकित्साशास्त्र की हिदायतों की कत्तई अवहेलना नहीं की जा सकती है । दुनिया की सभी सरकारों ने चिकित्सकों की इस सिफारिश का पूरा सम्मान किया, लेकिन इसके बावजूद सभी सरकारों ने सोशल डिस्टेंसिंग के उपायों को भी अपने गहन विचार का विषय बनाया ।
चीन ने वुहान और उसके आस-पास के क्षेत्र में सफलता से लॉक डाउन किया, पूरे देश को नहीं । दक्षिण कोरिया ने लॉक डाउन करने के बजाय शासन और जनता के बीच संपर्क पर बल देकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक किया । इटली और स्पेन में जब इसकी टेस्टिंग हुई, इसके पहले ही वह काफी लोगों में फैल गया था । बाद में लॉक डाउन आदि के उपाय करने पर भी उन देशों को काफी नुकसान उठाना पड़ा । ब्रिटेन सब जगह के अनुभवों को सामने रखते हुए पूर्ण लॉक डाउन के बजाय अन्य सभी उपायों से सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करवा रहा है । सभी सरकारों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही टेस्टिंग और उपचार के साधनों पर समान रूप से जोर देना शुरू कर दिया ।
इसी बीच अब अमेरिका कोरोना का सबसे बड़ा एपीसेंटर बन गया । भारत में भी सभी क्षेत्रों से कोरोना के संक्रमण की खबरें आने लगी । अमेरिका ने टेस्टिंग और इलाज पर जोर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग को सामाजिक जागरुकता के जरिये हासिल करने का रास्ता अपनाया । पर भारत में तो तो मोदी ने एक दिन के कथित जनता कर्फ्यू के बाद एक झटके में पूरे तीन हफ्तों के लिये पूरे देश में लॉक डाउन कर दिया । टेस्टिंग और उपचार के साधनों के विषय में वह दुनिया में सबसे पीछे की कतार में रहा ।
गौर करने की बात रही कि भारत में लॉक डाउन के हफ्ते भर के अनुभव के बाद भी अमेरिका ने अपने देश की संगीन परिस्थिति में भी बिल्कुल उलटी घोषणा कर दी कि वह लॉक डाउन का रास्ता नहीं अपनाएगा ।
भारत में देश-व्यापी लॉक डाउन के कारण जिस प्रकार की भारी सामाजिक अफरा-तफरी मची है, राष्ट्रीय हाइवे पर भूखे लोगों के सैलाब दिखाई देने लगे हैं, उसकी खबरें आज सारी दुनिया में फैल गई है। इस स्तर की सामाजिक अव्यवस्था भी दुनिया के देशों के लिए एक बड़ा सबक है और इसीलिए भारतीय उपमहादेश के ही बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल ने भी पूर्ण लॉक डाउन का रास्ता अपनाने से इंकार कर दिया है ।
कहना न होगा, मोदी जी ने सही इरादे से उठाए गए अपने गलत कदम से भारत को दुनिया के लिये गिनि पिग बना दिया, जैसा उन्होंने नोटबंदी के वक्त भी किया था । आज नोटबंदी की न मोदी कभी चर्चा करते है और न कोई और ।
यहीं पर आकर हम यह देख पाते हैं कि अमेरिका से आए हुए मोदी के सलाहकार या उनकी राजनीति के साथ मूलभूत रूप से जुड़ी हुई अमेरिका-परस्ती किस प्रकार मोदी शासन की नीतियों को भारतीय यथार्थ से काट देते हैं । कैसे वे भारत के लिये बेहद विनाशकारी साबित हो रही है । हमने जब मोदी सरकार की नीतियों और क्रियाकलापों पर अमेरिकी प्रभाव के पहलू का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ विश्लेषण करते हुए टिप्पणी की, तो उसमें कोई कांसपिरेसी थ्योरी नहीं, शुद्ध रूप से राजनीतिक क्रियाकलापों के पीछे विचारधारा की भूमिका की बात ही कही गई हैं ।