(जॉक लकान के मनोविश्लेषण के सिद्धांतों पर केंद्रित एक विमर्श की प्रस्तावना)
—अरुण माहेश्वरी
जाक लकान
(13 अप्रैल 1901 — 9 सितंबर 1981)
(2)
मनस्तात्त्विक विश्लेषण की शास्त्रीय पृष्ठभूमि
जब भी हम आदमी के मन या चित्त की कल्पना करते हैं, हमें उसका शुद्ध रूप एक अनादि, अनंत, अपौरुषेय शून्य ही जान पड़ता है । पूरी तरह से बोधमूलक । शास्त्रों में वेद को भी अनादि, अपौरुषेय और बोधात्मक कहा गया है । हमारे करपात्री जी महाराज तो वेद की नित्यता की चर्चा करते हुए भी उसे किसी घटना विशेष, इतिहास से जोड़ कर देखने की जरा सी कोशिश के भी सख्त विरोधी थे ।1(अनन्तश्रीस्वामिकरपात्रमहाराजाः, वेदार्थपारिजात:, खंड 2, पृष्ठ — 909) इस तरह उनके अनुसार मनुष्य के शुद्ध चित्त और वेद को एक दूसरे का पर्याय कहा जा सकता है । आदमी के चित्त की तस्वीर उसमें ज्ञान, इच्छा और क्रिया के जिस क्रम के योग से बनती है उसके प्रथम बिंदु ज्ञान, अर्थात् जानकारी के बारे में हमारे वाक्यपदीयकार भृतहरि कहते हैं कि —
“न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके य शब्दानुगमादृते” ।
अनुविद्धमिव ज्ञान सर्व शब्देन भासते ।।”
(अर्थात् लोक में ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं जो बिना शब्द की सहायता से हो सकता है । सारा ज्ञान शब्द के द्वारा प्रकाशित होता है ।)2(The Vakyapadiya, K Raghavan Pillai, Motilal Banarsidass, 1971, page – 28)
करपात्री जी महाराज वेद की नित्यता और अपौरुषेयता की जितनी भी चर्चा कर लें, वास्तविकता यही है कि वेदों की चर्चा भी इसी प्रकार अतीन्द्रीय शब्दात्मक सूक्ष्म ज्ञान विशेष के तौर पर ही की जाती है, भले ही वे वाचित हो या अवाचित (आम्नात या अनाम्नात), अखंड वेद के अंश के अनुकार मात्र ही हो । गौर करें —'शब्दात्मक सूक्ष्म ज्ञान', शब्दों में निरूपित सूक्ष्म ज्ञान । इसमें यह मान कर चला जाता है कि मनुष्य के लिये जगत उसके चित्त के अक्श के बाहर नहीं होता, जो शब्दाकार होता है और इसी वजह से अपौरुषेय अनादि प्राकृतिक ध्वनि के शब्दाकार को ही इस जगत का स्रष्टा कहा गया हैं । ॐ — जब इस धरती पर कुछ नहीं था, उस परम आदिम शून्य की ध्वनि का शब्दाकार, अर्थात्, मान्यताओं के अनुसार जगत का स्रष्टा ।
वाक्यपदीयकार भर्तृहरि कहते हैं —'शब्द ही ब्रह्म है' ; अर्थात आदमी के संदर्भ में उसके चित्त की संघटनकारी शब्दाकार निर्मितियों और जगत के निर्माण की प्रक्रिया में कोई भेद नहीं है । ब्रह्मांड यदि निरंतर विस्तारवान है तो मनुष्य का आत्म भी सदा विस्तार की एक अनंत प्रक्रिया में होता है । लेकिन फिर यह सवाल शेष रह जाता है कि अगर विस्तार है तो संकुचन भी है, तो फिर ठहराव भी होगा ही — इस प्रक्रिया के असंख्य रूप हो सकते हैं । यह सारा व्यापार किसी निश्चित लकीर से बंधा नहीं होता है । विघ्न के अतिरिक्त भटकाव भी होते हैं । तो आखिर इन सब अनंत भेदों की वजह क्या है ? और यह सवाल भी शेष रह जाता है कि सुनिश्चित आकारों. अर्थात् छवियों के चौखटों में बद्ध जगत निरंतर विस्तारवान, अर्थात गतिशील कैसे होता है ?
बहरहाल, भारतीय परंपरा में इसी चित्त को व्याख्यायित करने और उसे साधने के उपायों वाले शास्त्र का नाम है — तन्त्र । तन्त्र का अर्थ है विस्तार, आत्म के विस्तार की एक निश्चित क्रमिक प्रक्रिया । लोककल्याणकारी परम शिव (सत्य) के महाव्योम में आत्म के अंतहीन विस्तार का उपक्रम । परंतु जब आत्म के विस्तार की प्रक्रिया तय है, तब फिर संकुचन को भले आप परमशिव की स्वेच्छया स्वातंत्र्य क्रिया कह लें, लेकिन वह विस्तार की प्रक्रिया में एक वास्तविक रुकावट अथवा गतिरोध तो है ही । यहां तक कि इस प्रक्रिया में स्खलन और इसमें भटकाव की वास्तविकता से भी इंकार नहीं किया जा सकता है । इसीलिये, तंत्र यदि मनुष्य को उसके आत्म के विस्तार के पथ का दिग्दर्शन कराता है तो इसी क्रम में यह स्वाभाविक है कि वह उसके आत्म में ठहराव और भटकाव के बिंदुओं का संधान भी देता है । अर्थात तंत्र में मन है, मन का संकुचन और विस्तार है तो मन का भटकाव, और आधुनिक परिभाषा में, 'मनोरोग' (Psychosis) भी है।
भारतीय तंत्रशास्त्र ने हजारों साल के सूक्ष्म अवलोकनों से मन की इन सारी गतियों पर बेहद गहराई से दृष्टिपात करते हुए इसे परमार्थिक संदर्भों से जोड़ कर अपने आगम ग्रंथों से दर्शनशास्त्र के उन ऊंचे शिखरों तक पहुंचा दिया था, जहां से कश्मीरी शैवमत के शीर्षस्थ पुरुष अभिनवगुप्त (सन् 950-1016) ने विपुल आगम साहित्य पर टिके शैवदर्शन से हजारों सालों की अन्य सभी भारतीय दर्शन की धाराओं को बौना कर दिया था । यह एक प्राचीन तांत्रिक परंपरा का दार्शनिक उत्तरण है । विभिन्न धाराओं के तांत्रिक व्यवहारों और सिद्धांतों से पेश होने वाली चिंतन की समस्याओं का एक तार्किक दार्शनिक समाधान ।
तंत्र की तरह ही पश्चिम में मनोविश्लेषण का भी एक चिंतन के रूप में विज्ञान, राजनीति और दर्शनशास्त्र से गहरा नैसर्गिक संबंध है । चिंतन की इन अलग-अलग धाराओं के व्यवहारिक रूपों में कितना ही भेद क्यों न हो, पर इनमें एक गहरा अन्तरसंबंध है, बल्कि कहीं कहीं तो ये स्पष्ट तौर पर परस्पर की सीमाओं का उल्लंघन करते हैं । जैसे तंत्र का पूरा महल शैवागमों, स्पंद और प्रत्यभिज्ञादर्शन को मिला कर ही तैयार होता है, उसी प्रकार चिंतन की एकान्विति के अन्तरगत लिखने के क्षण, परिवर्तन के क्षण या अनुभव के क्षण के बीच एक संबंध हमेशा देखा जा सकता है । ये चिंतन की अलग-अलग श्रेणियां हैं । इनमें अलगाव है तो एकसूत्रता भी हैं ।
मसलन्, विज्ञान और राजनीति को ही लिया जाए । ये दोनों पूरी तरह से अलग-अलग चिंतन-क्षेत्र हैं, इसलिये क्योंकि भौतिकी के प्रयोगों का अंत ऐसी कृत्रिम निर्मितियों में होता है, जिन्हें दोहराया जा सकता है । गणितीय लेखन भी इसी प्रकार प्रयोगों से मेल खाता है जिसमें किसी भी समीकरण का हमेशा एक ही परिणाम होता है । गणितीय समीकरणों में यह समानता उसमें शुरू से ही अन्तरग्रथित होती है । लेकिन राजनीति में लेखन और प्रयोग के बीच संबंध इससे बिल्कुल भिन्न होता है । कोई भी राजनीतिक परिस्थिति हमेशा स्वयं में अलग और अनोखी होती है । उसे कभी हूबहू दोहराया नहीं जा सकता है । इसीलिये राजनीतिक लेखन, उनकी दिशा और निर्देश, अपनी सीमा में ही सही होते हैं, हर राजनीतिक घटना का अपना निजी भुवन होता है, इसमें कभी किसी अन्य घटना का दोहराव नहीं हुआ करता है । जब भी किसी राजनीतिक लेखन में दोहराव दिखाई देता है, वह कोरा शब्दाडंबर और खोखला दिखाई देने लगता है । यह स्वयं में एक कसौटी भी है जिसके आधार पर सच्चे राजनीतिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक नेताओं के बीच फर्क किया जा सकता है । सच्चे राजनीतिक कार्यकर्ता यह मान कर चलते है कि कोई भी परिस्थिति दोहराई नहीं जा सकती है, जबकि चालू प्रकार के राजनीतिक नेता मान्य बातों का पिष्टपेषण करते हुए ही भाषणबाजी किया करते हैं । सच्चे राजनीतिक कार्यकर्ता हमेशा एक अलग परिस्थिति के बारे में सोचते है । फलत: राजनीतिक चिंतन वैज्ञानिक चिंतन से पूरी तरह अलग होता है । राजनीति एक खास और न दोहराई जा सकने वाली संभावना की बात करती है । विज्ञान एक जरूरत से पैदा होता है, उसके समाधान के सूत्र तैयार करता है और उसके दोहराव के उपकरणों का निर्माण करता है ।
मनोविश्लेषणात्मक चिंतन के बारे में भी यही बात लागू होती है कि उसमें होने वाली अनुभूति विज्ञान की तरह की नहीं होती है । यह अलग-अलग आदमी के विश्लेषण और चिकित्सा के अनुभव पर टिका होता है और कोई भी आदमी दूसरे की प्रतिलिपि नहीं होता । मनोविश्लेषणात्मक चिंतन में सैद्धांतिक लेखन और चिकित्सकीय परिस्थिति के बीच संबंध में दोहराव की तरह की कोई कृत्रिम बात नहीं होती है । इस अर्थ में कह सकते हैं कि मनोविश्लेषण वैज्ञानिक चिंतन के बजाय राजनीतिक चिंतन के ज्यादा करीब है । मनोविश्लेषण और राजनीति के बीच समानता का एक और सूत्र है ज्ञान के सामूहिक संकलन की जरूरत । राजनीति के लिये संगठन जरूरी है, इसी प्रकार विश्व में मनोविश्लेषकों के भी हमेशा एसोशियेसन रहे हैं । इन क्षेत्रों के अनुभवों की अद्वितीयता की जांच हमेशा अन्यों के साथ मिल कर एक प्रकार से मनुष्यों के ही आत्मगत स्तर पर की जा सकती है । दोनों में विषय की सामूहिक समझ महत्वपूर्ण होती है ।
बहरहाल, जैसे चिंतन के रूप में राजनीति का लक्ष्य चिंतन मात्र के सिवाय कुछ नहीं होता है ; अर्थात् अद्वितीय परिस्थितियों के रूपांतरण को चिंतन का विषय बनाना, इसमें सिद्धांत और व्यवहार के बीच के भेद को दूर करना । विज्ञान में भी न्यूटन और आइंस्टीन का लक्ष्य विचार की समस्याओं के समाधान के अलावा और कुछ नहीं था । किसी भी बड़े कलाकार का लक्ष्य चिंतन को ही एक कृति का रूप देना होता है, और कुछ नहीं । राजनीति का लक्ष्य राजनीति की समस्याओं का समाधान करना होता है, उन समस्याओं का जिन्हें राजनीति खुद अपने सामने खड़ा करती है । उसी प्रकार एक स्तर पर जा कर मनोविश्लेषण का लक्ष्य भी निःस्वार्थ चिंतन हो जाता है ।
इस लिहाज से पश्चिम में मनोविश्लेषण की आधुनिक धारा के जनक सिगमेंड फ्रायड और उनके श्रेष्ठ शिष्य जॉक लकान के कामों का लक्ष्य भी अन्ततः सिर्फ रोगी के रोग का निदान नहीं रह गया था । उनका मूल लक्ष्य समग्र मनुष्य के बारे में बिल्कुल अलग से विचार करने का था : वह मनुष्य जो एक तरफ भाषा से, अपने सांस्कृतिक परिवेश के दबावों से जूझता है और दूसरी ओर खुद की वासनाओं, ऐंन्द्रिक इच्छाओं और कामुकता से भी जूझता है । अर्थात् भाषा और शरीर दोनों से । मनोविश्लेषण जब मनोरोगी के लक्षणों को दूर करने तक सीमित रहने के बजाय मनुष्य की नई संभावनाओं की तलाश की दिशा में बढ़ जाता है, वह अपने कथित भुवन की सीमा को लांघ कर चिंतन के भुवन में प्रवेश कर जाता है ; आदमी की संरचना की ‘सामान्य’ क्रियाशीलता का अध्ययन बन जाता है । और चिंतन के इन दो स्तरों की, बल्कि दो विधाओं के बीच संबंध की समस्या हमेशा एक तीसरी, दर्शनशास्त्र की जमीन पर ही समाधित होती है ।
इसी बिंदु पर हम कह सकते हैं कि जैसे शैवागमों और स्पंद के सिद्धांत और व्यवहार की एक सहज अन्विती प्रत्यभिज्ञा दर्शन में दिखाई देती है, उसी प्रकार भारतीय तंत्र के शास्त्र के साथ पश्चिमी मनोविश्लेषण के बीच भी एक सादृश्यता देखी जा सकती है ।
शैव दर्शन को भोग और मोक्ष दोनों, अर्थात मनुष्य के बाह्य क्रियाकलापों और अन्तर के कार्यों, दोनों से जोड़ कर वस्तुतः उस जमीन को तैयार कर दिया गया था जिसे पश्चिमी दर्शनशास्त्र की दीर्घ परंपरा के उपरांत हम कार्ल मार्क्स (5 मई 1818 — 14 मार्च 1883) के जरिये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के रूप में चरितार्थ होते देखते हैं । सच्चा भौतिकवाद । यह न पदार्थ की प्राथमिकता पर टिका है और न ही पदार्थ को प्रथम सिद्धांत मानने पर । इस भौतिकवाद की सच्चाई भौतिक वस्तु की, यथार्थ की स्वतंत्र उपस्थिति से प्रमाणित नहीं होती है । बल्कि, यह अन्तर और बाह्य के द्वंद्व, उनके बीच की दरारों और इनसे बनने वाले यथार्थ के अवभास की धारणा पर टिकी है । इसका संबंध यथार्थ में दिखाई देने वाली उन दरारों के साथ होता है, जिनके बीच से यथार्थ लगातार बदलता रहता है । जीवन परिवर्तनशील है, और जीवन की गति की यह सच्चाई इन दरारों के स्फोटों से ही निरंतर आकार लेती है । द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इसी परिवर्तनशील यथार्थ का दर्शन है । यह मनुष्य के अन्तर-बाह्य का दर्शन है ; इतिहास के संदर्भ में पौर्वापर्य विवेचन की विचारधारा, वस्तु के आगे और पीछे, दोनों को समेट कर चलने वाले, अर्थात उसके गतिशील रूप का विवेचन करने वाली विचारधारा । तंत्र में उत्पलदेव का प्रत्यभिज्ञा दर्शन अर्थात् त्रिक दर्शन शैवमत की क्रम और कुल की विवेचन-धाराओं से इसी प्रकार अविभाज्य है ।
किसी भी परिघटना में क्रम की एक श्रृंखला तैयार होती है । उस श्रृंखला की हर कड़ी के अंदर के सूक्ष्म छिद्रों, दरारों से हमेशा किसी चमत्कार, सर्जनात्मक स्फोट अथवा ऐतिहासिक परिवर्तन की घटना के क्रांतिकारी बिंदु प्रकाशित होते हैं । इन्हें लक्षण (symptom) कहा जाता है । मार्क्स ने उन्हें पकड़ कर ही सामाजिक संबंधों के एक महाजाल और उसमें परिवर्तन के तत्वों की सिनाख्त करके उसके नियमों का एक ऐसा क्रमवार सिद्धांत पेश किया जिसमें तमाम आकस्मिकताओं की भूमिका को भी साफ देखा जा सकता है । इसीलिये मार्क्स को फ्रांसीसी मनोविश्लेषक जॉक लकान ने बिल्कुल सही लक्षणों का आविष्कारक कहा है । जॉक लकान ने अपने सेमिनार XX में फ्रायड-लकान के संबंध की तुलना मार्क्स-एंगेल्स के बीच संबंध से की हैं । उनका संकेत साफ था कि इस प्रकार से दो चिंतन क्षेत्रों के बीच तुलना करना संभव है, बल्कि, इससे वे परस्पर को शिक्षित और समृद्ध भी कर सकते हैं ।





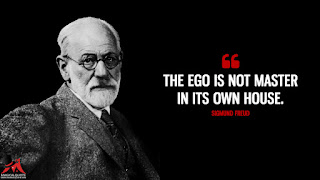





कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें