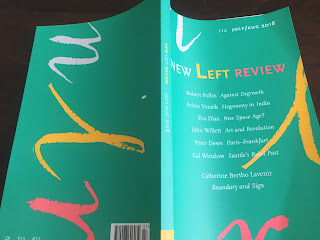—अरुण माहेश्वरी
कल (27 अक्तूबर 2018 को) ही एनडी टीवी पर यशवंत सिन्हा का एक साक्षात्कार देख रहा था । उसमें उनसे पूछा गया कि उनका अति शिक्षित बेटा जयंत सिन्हा जब गाय के नाम पर हत्या करने वालों की जमानत से रिहाई पर जेल के फाटक पर उन्हें माला पहनाने पहुंचा तो उसे देख कर उन्हें कैसा लगा ?
इसपर यशवंत सिन्हा ने कहा कि उन्हें बुरा लगा, लेकिन इससे हमारा उनसे जो पारिवारिक संबंध है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है । उनके विचार मेरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन घर में हम पिता-पुत्र ही हैं ।
हमारा सवाल है कि यह पिता-पुत्र का संबंध आखिर क्या चीज है ? क्या यह सिर्फ एक प्रकार का जैविक संबंध होता है, या व्यापक सामाजिक संदर्भ में इसके कुछ दूसरे मायने भी होते हैं ? पुत्र के साथ पिता के संबंध को अगर महज जैविक ही मान लिया जाए, तो आज के आधुनिक जगत में उसे छोटा करते-करते महज पिता के शुक्राणु तक में सीमित किया जा सकता है । टेस्ट ट्यूब बेबी तो वही है ।
हमारे सामने समस्या दूसरी है । पिता के साथ पुत्र के ऐसे संबंध की जिसे सामान्य तौर पर पीढ़ियों के बीच का व्यवधान कहा जाता है । इसमें मान लिया जाता है कि पिता की तुलना में पुत्र नई पीढ़ी का युवा होने के नाते कहीं ज्यादा आगे की सोच का अधिकारी है, और इसीलिये वह परिवार के ढांचे में पिता की स्वामी वाली उपस्थिति को स्वीकारने से इंकार करता है ।
इस मामले में आज के युग में उदार विचारों का पिता एक समय के बाद परिवार की बागडोर वयस्क पुत्र को सौंप कर अपने स्वामित्व वाले स्थान को त्याग दिया करता है । लेकिन यह हमारी समस्या का समाधान नहीं है । सक्षम और चेतना संपन्न पिता मृत्यु-पर्यंत अपने स्वत्व के, अपनी स्वतंत्र अस्मिता के बोध को कभी न छोड़ पाने के कारण ही अक्सर पुत्र के अहम के लिये एक प्रतिद्वंद्विता और डर का विषय बना रहता है । पुत्र उससे टकराते हुए ही अपने स्वातंत्र्य के बोध को पाता है ।
इसीलिये जब यशवंत सिन्हा परिवार में पुत्र के साथ अपने संबंधों को सामान्य कहते हैं तो हमारा मन उसे स्वीकारता भी है और नहीं भी स्वीकारता है । हमें लगता है कि पिता-पुत्र के संबंधों को समझने के लिये पिता को महज एक जैविक सत्ता के बजाय एक समाज की पूरी आत्मिक संरचना के संदर्भ में एक सांस्कृतिक, प्रतीकात्मक सत्ता के रूप में देखने की जरूरत है ।
संरचनामूलक मानवशास्त्री लेवी स्ट्रास ने बताया था कि परिवारों का स्वरूप किसी एकल परिवार मात्र से नहीं जाना जा सकता है । इसमें पत्नी के जरिये उसके मायके के लोग गुथे होते हैं, एक प्रकार से पूरा कुनबा और गोत्र शामिल हो जाता है । समाजशास्त्री मार्शेल मौस, जो संस्कृत के पंडित भी थे, अपनी पुस्तक 'गिफ्ट' में, जिसमें वे महाभारत और भारतीय नीति शास्त्र के धर्म, अर्थ, काम के पहलू का भी जिक्र करते हैं, कहते हैं कि समाज बनता है और एकजुट रहता है आपस में और अलग-अलग पीढ़ियों के बीच भी उपहारों के आदान-प्रदान के निरंतर चक्र से । ये उपहार संपत्तियों और सामानों के हो सकते हैं और व्यक्तियों के भी । इनसे ही समाज को उसका सांस्कृतिक प्रतीकात्मक स्वरूप मिलता है । इसीलिये मौस ने 'प्रदान' को ही एक प्रतीकात्मक क्रिया के रूप में देखा था, क्या प्रदान किया गया उसे महत्वपूर्ण नहीं माना ।1
शादी में भी एक प्रकार से व्यक्तियों का आदान-प्रदान होता है, जिसके आयोजन में सिर्फ निकट के संबंधी और माता-पिता नहीं, पूरा समुदाय जुड़ जाया करता है । कहना न होगा, इसके जरिये आदमी और औरत एक पूरी समाज की प्रतीकात्मक श्रृंखला से जुड़ जाते हैं । मनोविश्लेषक जॉक लकान कहते हैं कि एक वास्तविक और जैविक पिता को इन प्रतीकात्मक ढांचों से अलग करके देखना चाहिए । आदमी और औरत के संबंध को वास्तव में समाज के प्रतीकात्मक ढांचे तय करते हैं । इसीलिये परिवार में पिता महज एक नाम होता है, उसकी भूमिका एक जैविक व्यक्ति की भूमिका के बजाय प्रतीकात्मक नाम की होती है ।
और जब कोई पिता की इस प्रतीकात्मक उपस्थिति से पूरी तरह से इंकार करता हैं, तब उसके लिये पिता के जैविक तौर पर मौजूद रहने के बावजूद क्या उसकी मौजूदगी का कोई विशेष अर्थ रह जाता है ?
यशवंत सिन्हा सच कह रहे थे कि अपने कट्टर संघी पुत्र से परिवार में उनके संबंधों पर कोई फर्क नहीं आया है, लेकिन इतना साफ है कि जयंत सिन्हा के जीवन में उनके पिता की प्रतीकात्मक उपस्थिति, जो जैविक की तुलना में दरअसल कहीं ज्यादा वास्तविक होती है, उसमें जरूर एक दरार पड़ी है । इस विषय ने हमारा ध्यान खास तौर पर इसलिये खींचा क्योंकि पिता-पुत्र के संबंधों की ऐसी मृत परिणति को हमने अपने निकट के अनेक लेखकों के परिवारों में देखा है । लेखकों के आदर्शों से मुक्त हो कर ही अक्सर उनके पुत्र भौतिक-आत्मिक जीवन में अपनी सफलताओं के रास्ते तैयार किया करते हैं ।
1.“We should come out of ourselves and regard the duty of giving as a liberty, for in it lies no risk….Give as much as you receive and all is for the best…It is our fortune that all is not couched in terms of purchase and sale…Our morality is not solely commercial…It is some thing other than utility which makes goods circulate in these multifarious and fairly enlightened societies. Clans, age groups and seces, in view of many relationships ensuing from contacts between them, are in a state of perpetual economic effervescence which has little about it that is materialistic ; it is much less prosaic than our sale and purchase, hire of services and speculations. (MARCEL MAUSS ; THE GIFT : Forms and Functions of Exchangein Archaic Societies ; COHEN & WEST LTD, 1966 ; Page – 69-70)
कल (27 अक्तूबर 2018 को) ही एनडी टीवी पर यशवंत सिन्हा का एक साक्षात्कार देख रहा था । उसमें उनसे पूछा गया कि उनका अति शिक्षित बेटा जयंत सिन्हा जब गाय के नाम पर हत्या करने वालों की जमानत से रिहाई पर जेल के फाटक पर उन्हें माला पहनाने पहुंचा तो उसे देख कर उन्हें कैसा लगा ?
इसपर यशवंत सिन्हा ने कहा कि उन्हें बुरा लगा, लेकिन इससे हमारा उनसे जो पारिवारिक संबंध है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है । उनके विचार मेरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन घर में हम पिता-पुत्र ही हैं ।
हमारा सवाल है कि यह पिता-पुत्र का संबंध आखिर क्या चीज है ? क्या यह सिर्फ एक प्रकार का जैविक संबंध होता है, या व्यापक सामाजिक संदर्भ में इसके कुछ दूसरे मायने भी होते हैं ? पुत्र के साथ पिता के संबंध को अगर महज जैविक ही मान लिया जाए, तो आज के आधुनिक जगत में उसे छोटा करते-करते महज पिता के शुक्राणु तक में सीमित किया जा सकता है । टेस्ट ट्यूब बेबी तो वही है ।
हमारे सामने समस्या दूसरी है । पिता के साथ पुत्र के ऐसे संबंध की जिसे सामान्य तौर पर पीढ़ियों के बीच का व्यवधान कहा जाता है । इसमें मान लिया जाता है कि पिता की तुलना में पुत्र नई पीढ़ी का युवा होने के नाते कहीं ज्यादा आगे की सोच का अधिकारी है, और इसीलिये वह परिवार के ढांचे में पिता की स्वामी वाली उपस्थिति को स्वीकारने से इंकार करता है ।
इस मामले में आज के युग में उदार विचारों का पिता एक समय के बाद परिवार की बागडोर वयस्क पुत्र को सौंप कर अपने स्वामित्व वाले स्थान को त्याग दिया करता है । लेकिन यह हमारी समस्या का समाधान नहीं है । सक्षम और चेतना संपन्न पिता मृत्यु-पर्यंत अपने स्वत्व के, अपनी स्वतंत्र अस्मिता के बोध को कभी न छोड़ पाने के कारण ही अक्सर पुत्र के अहम के लिये एक प्रतिद्वंद्विता और डर का विषय बना रहता है । पुत्र उससे टकराते हुए ही अपने स्वातंत्र्य के बोध को पाता है ।
इसीलिये जब यशवंत सिन्हा परिवार में पुत्र के साथ अपने संबंधों को सामान्य कहते हैं तो हमारा मन उसे स्वीकारता भी है और नहीं भी स्वीकारता है । हमें लगता है कि पिता-पुत्र के संबंधों को समझने के लिये पिता को महज एक जैविक सत्ता के बजाय एक समाज की पूरी आत्मिक संरचना के संदर्भ में एक सांस्कृतिक, प्रतीकात्मक सत्ता के रूप में देखने की जरूरत है ।
संरचनामूलक मानवशास्त्री लेवी स्ट्रास ने बताया था कि परिवारों का स्वरूप किसी एकल परिवार मात्र से नहीं जाना जा सकता है । इसमें पत्नी के जरिये उसके मायके के लोग गुथे होते हैं, एक प्रकार से पूरा कुनबा और गोत्र शामिल हो जाता है । समाजशास्त्री मार्शेल मौस, जो संस्कृत के पंडित भी थे, अपनी पुस्तक 'गिफ्ट' में, जिसमें वे महाभारत और भारतीय नीति शास्त्र के धर्म, अर्थ, काम के पहलू का भी जिक्र करते हैं, कहते हैं कि समाज बनता है और एकजुट रहता है आपस में और अलग-अलग पीढ़ियों के बीच भी उपहारों के आदान-प्रदान के निरंतर चक्र से । ये उपहार संपत्तियों और सामानों के हो सकते हैं और व्यक्तियों के भी । इनसे ही समाज को उसका सांस्कृतिक प्रतीकात्मक स्वरूप मिलता है । इसीलिये मौस ने 'प्रदान' को ही एक प्रतीकात्मक क्रिया के रूप में देखा था, क्या प्रदान किया गया उसे महत्वपूर्ण नहीं माना ।1
शादी में भी एक प्रकार से व्यक्तियों का आदान-प्रदान होता है, जिसके आयोजन में सिर्फ निकट के संबंधी और माता-पिता नहीं, पूरा समुदाय जुड़ जाया करता है । कहना न होगा, इसके जरिये आदमी और औरत एक पूरी समाज की प्रतीकात्मक श्रृंखला से जुड़ जाते हैं । मनोविश्लेषक जॉक लकान कहते हैं कि एक वास्तविक और जैविक पिता को इन प्रतीकात्मक ढांचों से अलग करके देखना चाहिए । आदमी और औरत के संबंध को वास्तव में समाज के प्रतीकात्मक ढांचे तय करते हैं । इसीलिये परिवार में पिता महज एक नाम होता है, उसकी भूमिका एक जैविक व्यक्ति की भूमिका के बजाय प्रतीकात्मक नाम की होती है ।
और जब कोई पिता की इस प्रतीकात्मक उपस्थिति से पूरी तरह से इंकार करता हैं, तब उसके लिये पिता के जैविक तौर पर मौजूद रहने के बावजूद क्या उसकी मौजूदगी का कोई विशेष अर्थ रह जाता है ?
यशवंत सिन्हा सच कह रहे थे कि अपने कट्टर संघी पुत्र से परिवार में उनके संबंधों पर कोई फर्क नहीं आया है, लेकिन इतना साफ है कि जयंत सिन्हा के जीवन में उनके पिता की प्रतीकात्मक उपस्थिति, जो जैविक की तुलना में दरअसल कहीं ज्यादा वास्तविक होती है, उसमें जरूर एक दरार पड़ी है । इस विषय ने हमारा ध्यान खास तौर पर इसलिये खींचा क्योंकि पिता-पुत्र के संबंधों की ऐसी मृत परिणति को हमने अपने निकट के अनेक लेखकों के परिवारों में देखा है । लेखकों के आदर्शों से मुक्त हो कर ही अक्सर उनके पुत्र भौतिक-आत्मिक जीवन में अपनी सफलताओं के रास्ते तैयार किया करते हैं ।
1.“We should come out of ourselves and regard the duty of giving as a liberty, for in it lies no risk….Give as much as you receive and all is for the best…It is our fortune that all is not couched in terms of purchase and sale…Our morality is not solely commercial…It is some thing other than utility which makes goods circulate in these multifarious and fairly enlightened societies. Clans, age groups and seces, in view of many relationships ensuing from contacts between them, are in a state of perpetual economic effervescence which has little about it that is materialistic ; it is much less prosaic than our sale and purchase, hire of services and speculations. (MARCEL MAUSS ; THE GIFT : Forms and Functions of Exchangein Archaic Societies ; COHEN & WEST LTD, 1966 ; Page – 69-70)